RPSC 2nd Grade Paper Solution
1. निम्नलिखित में से कौनसा पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित है ?
इस प्रश्न का सही उत्तर है: (3) उड़िया का पठार, भोराठ का पठार, मुकुन्दरा की पहाड़ियाँ।
यह क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर राजस्थान की भौगोलिक विशेषताओं की स्थिति के अनुसार है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं:
1. उड़िया का पठार
उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊँचा पठार है, जो सिरोही जिले में माउंट आबू के पास स्थित है। यह अरावली पर्वतमाला के दक्षिणी भाग में आता है और इसकी ऊँचाई लगभग 1360 मीटर है। पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए, यह सबसे पहले आता है।
2. भोराठ का पठार
भोराठ का पठार गोगुन्दा (उदयपुर) और कुम्भलगढ़ (राजसमंद) के बीच स्थित है। यह अरावली की पहाड़ियों में स्थित एक महत्वपूर्ण पठारी क्षेत्र है। यह उड़िया के पठार के पूर्व में स्थित है, लेकिन मुकुन्दरा की पहाड़ियों से पश्चिम में है।
3. मुकुन्दरा की पहाड़ियाँ
मुकुन्दरा की पहाड़ियाँ राजस्थान के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में कोटा और झालावाड़ जिले के बीच स्थित हैं। ये पहाड़ियाँ हाड़ौती के पठार का हिस्सा हैं और विंध्य पर्वतमाला का विस्तार हैं। ये उड़िया और भोराठ के पठार से बहुत पूर्व में स्थित हैं।
इस प्रकार, पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है: उड़िया का पठार → भोराठ का पठार → मुकुन्दरा की पहाड़ियाँ।
RPSC 2nd Grade 2025 paper Solution
2. 2011 की जनगणना में, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का शिशु लिंगानुपात अन्य जिलों की तुलना में सर्वाधिक था ?
2011 की जनगणना के अनुसार, राजस्थान में बाँसवाड़ा जिले का शिशु लिंगानुपात (0-6 वर्ष) अन्य जिलों की तुलना में सबसे अधिक था।
राजस्थान में शिशु लिंगानुपात (2011)
2011 की जनगणना के आँकड़ों के अनुसार, राजस्थान का औसत शिशु लिंगानुपात 888 था। लेकिन जिलों के आधार पर इसमें काफी भिन्नता थी।
बाँसवाड़ा: 934 (सर्वाधिक)
प्रतापगढ़: 933
भीलवाड़ा: 928
डूंगरपुर: 922
इन आँकड़ों के आधार पर, बाँसवाड़ा जिले का शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक था, जो दर्शाता है कि यह जिला बालिकाओं के जन्म और जीवन के प्रारंभिक वर्षों में लैंगिक समानता के मामले में बेहतर स्थिति में था।
3. निम्नलिखित में से कौनसे जिले उनके सामान्य वार्षिक वर्षा के आधार पर सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित हैं ?
सही अवरोही क्रम (घटते क्रम) (1) बाँसवाड़ा, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़ है।
वार्षिक वर्षा का भौगोलिक वितरण
राजस्थान में वार्षिक वर्षा की मात्रा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में काफी भिन्न होती है, और यह मुख्य रूप से राज्य की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करती है। सामान्यतः, दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा होती है, जबकि उत्तर-पश्चिमी राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है।
बाँसवाड़ा: यह जिला राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में स्थित है, जिसे “सौ द्वीपों का शहर” भी कहा जाता है। यह मानसूनी हवाओं के सीधे मार्ग में आता है और यहाँ राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है, जिसकी औसत वार्षिक मात्रा 900 मिमी से अधिक होती है।
भीलवाड़ा: यह राजस्थान के मध्य-दक्षिणी भाग में स्थित है। यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा बाँसवाड़ा की तुलना में कम होती है, लेकिन हनुमानगढ़ से अधिक होती है। यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा 600-700 मिमी के बीच होती है।
हनुमानगढ़: यह राजस्थान के उत्तरी भाग में स्थित है। यह क्षेत्र थार रेगिस्तान के करीब है और यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा 300 मिमी से भी कम होती है।
इन जिलों की वार्षिक वर्षा के आधार पर, अवरोही क्रम (सबसे अधिक से सबसे कम) इस प्रकार है:
बाँसवाड़ा > भीलवाड़ा > हनुमानगढ़
यह क्रम इस तथ्य को दर्शाता है कि राजस्थान में वर्षा की मात्रा दक्षिण-पूर्व से उत्तर-पश्चिम की ओर घटती जाती है।
4. “नेक्स्ट जेन टेक्सटाइल पार्क” राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है?
“नेक्स्ट जेन टेक्सटाइल पार्क” राजस्थान के पाली जिले में स्थित है। यह एक विशेष प्रयोजन वाहन (Special Purpose Vehicle) के तहत विकसित किया गया एक एकीकृत कपड़ा पार्क है।
यह पार्क पाली शहर से लगभग 5 किमी दूर सरदार समंद रोड पर 94 एकड़ भूमि में फैला हुआ है।
यह मुख्य रूप से कपड़े की छपाई और रंगाई की गतिविधियों पर केंद्रित है।
पाली को पहले से ही कपड़ा उद्योग का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है, और यह पार्क इस क्षेत्र में इस उद्योग को और बढ़ावा देने का काम कर रहा है।
5. इण्डिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे -कम कुल वनावरण क्षेत्र वाले जिलों का र्युग्म कौनसा है ?
वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार, राजस्थान के सबसे कम कुल वनावरण क्षेत्र वाले जिलों का युग्म (4) चूरू तथा जोधपुर है।
इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट (ISFR) 2023
वन सर्वेक्षण रिपोर्ट (ISFR) भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India) द्वारा हर दो साल में जारी की जाती है। यह रिपोर्ट देश के वन और वृक्ष संसाधनों का आकलन प्रस्तुत करती है। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान के विभिन्न जिलों में वनावरण की स्थिति इस प्रकार है:
सबसे कम वनावरण वाले जिले: राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में स्थित जिलों में वनावरण सबसे कम है। इस सूची में चूरू और जोधपुर शीर्ष पर हैं, जहाँ वनावरण का क्षेत्र अत्यंत न्यूनतम है।
सबसे अधिक वनावरण वाले जिले: इसके विपरीत, उदयपुर, अलवर, और प्रतापगढ़ जैसे जिले, जो राज्य के दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी भाग में स्थित हैं, में सर्वाधिक वनावरण पाया जाता है।
यह डेटा इस बात की पुष्टि करता है कि राज्य के पश्चिमी भाग में रेगिस्तानी जलवायु के कारण वनों की कमी है, जबकि दक्षिणी और पूर्वी भाग में अधिक अनुकूल परिस्थितियों के कारण वनावरण का घनत्व अधिक है।
6. पशुगणना – 2019 के अनुसार, राजस्थान में भारत के ऊँटों का प्रतिशत है –
पशुगणना 2019 के अनुसार, राजस्थान में भारत के कुल ऊँटों का 84.43% हिस्सा है।
यह आँकड़ा दर्शाता है कि देश में सबसे अधिक ऊँटों की आबादी राजस्थान में है। यह राज्य की भौगोलिक स्थिति और रेगिस्तानी जलवायु के कारण है, जहाँ ऊँट परिवहन और कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण जानवर रहा है।
मुख्य बिंदु:
देश में ऊँटों की कुल संख्या: 2019 की पशुगणना के अनुसार, भारत में ऊँटों की कुल संख्या 2.5 लाख है।
राजस्थान में ऊँटों की संख्या: इस कुल संख्या में से, अधिकांश ऊँट राजस्थान में पाए जाते हैं।
पिछले दशक में कमी: हालांकि, 2012 की पिछली पशुगणना की तुलना में 2019 में ऊँटों की संख्या में 37.1% की कमी दर्ज की गई है। इस कमी के मुख्य कारणों में उनके उपयोग में कमी, चरवाहों की संख्या में गिरावट और तस्करी शामिल हैं।
7. निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर नदी की पहचान कीजिए –
दी गई विशेषताओं के आधार पर, यह नदी खारी है।
खारी नदी की विशेषताएँ
उद्गम: खारी नदी का उद्गम स्थल राजसमंद जिले में स्थित बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से होता है।
सहायक नदी: यह बनास नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह भीलवाड़ा जिले में नन्दराय के निकट बनास नदी से मिलती है।
कुल लम्बाई: इसकी अनुमानित लम्बाई 80 किमी है।
अपवाह क्षेत्र: यह मुख्य रूप से राजसमंद, भीलवाड़ा और अजमेर जिलों में बहती है।
यह नदी अजमेर जिले में स्थित नारायण सागर बाँध का मुख्य स्रोत भी है, जिसे अजमेर की जीवन रेखा कहा जाता है।
8. निम्नलिखित (वन्यजीव अभयारण्य – अवस्थित) में से कौनसा सही सुमेलित हैं ?
दिए गए विकल्पों में से, (3) सवाई मानसिंह – सवाई माधोपुर सही सुमेलित है।
वन्यजीव अभयारण्यों का सही स्थान
सवाई मानसिंह वन्यजीव अभयारण्य: यह अभयारण्य सवाई माधोपुर जिले में स्थित है और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बफर जोन का हिस्सा है।
भैंसरोड़गढ़ वन्यजीव अभयारण्य: यह चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, न कि भीलवाड़ा में। यह चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित है।
शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य: यह बारां जिले में स्थित है, न कि जैसलमेर में। यह अभयारण्य परवन नदी के तट पर स्थित है।
जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य: यह कोटा जिले में स्थित है। यह चंबल नदी के किनारे पर स्थित है और मगरमच्छों के संरक्षण के लिए जाना जाता है।
9. एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स एट ए ग्लान्स 2023 (भारत) के अनुसार, निम्नलिखित (फसल-भारत के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान) में से कौनसा सुमेलित नहीं है ?
उपर्युक्त विकल्पों में से, (3) मूंगफली 18.76% सुमेलित नहीं है।
एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लान्स 2023 के अनुसार, राजस्थान का भारत के कुल मूंगफली उत्पादन में योगदान 18.76% नहीं, बल्कि 10.66% है।
अन्य विकल्प इस रिपोर्ट के अनुसार सही सुमेलित हैं:
बाजरा: राजस्थान भारत का सबसे बड़ा बाजरा उत्पादक राज्य है, जिसका कुल उत्पादन में 40.66% हिस्सा है।
रेपसीड और सरसों: राजस्थान भारत में रेपसीड और सरसों का भी सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसका योगदान 46.13% है।
ग्वार: ग्वार के उत्पादन में भी राजस्थान का एकाधिकार है। भारत के कुल उत्पादन का 90.36% राजस्थान में होता है।
इस प्रकार, मूंगफली का आँकड़ा सही नहीं है।
10. जनगणना 2011 के अनुसार, शहरी राजस्थान में 2001-2011 तक दशकीय परिवर्तन निम्न में से किस जिले में सबसे कम था ?
जनगणना 2011 के अनुसार, 2001-2011 के दौरान डूंगरपुर जिले में शहरी जनसंख्या में दशकीय परिवर्तन (Decadal Change) सबसे कम था।
शहरी जनसंख्या में दशकीय परिवर्तन
2001 से 2011 के बीच, राजस्थान की कुल शहरी जनसंख्या में 3.46% की वृद्धि हुई। हालाँकि, विभिन्न जिलों में यह वृद्धि दर अलग-अलग थी।
डूंगरपुर: इस जिले में शहरीकरण की दर बहुत धीमी थी, जिसके कारण शहरी जनसंख्या में सबसे कम वृद्धि दर्ज की गई।
अलवर: अलवर एक तेजी से विकसित हो रहा जिला है, जिसका औद्योगिक विकास भी अधिक है। इसलिए यहाँ शहरी जनसंख्या में वृद्धि दर अधिक थी।
हनुमानगढ़: यह जिला कृषि प्रधान होने के बावजूद भी, शहरों में जनसंख्या वृद्धि की दर डूंगरपुर से काफी अधिक थी।
प्रतापगढ़: इस जिले का गठन 2008 में हुआ था, लेकिन फिर भी यहाँ शहरी जनसंख्या में वृद्धि दर डूंगरपुर से अधिक थी।
अतः, इन चारों विकल्पों में से, डूंगरपुर का शहरी जनसंख्या में दशकीय परिवर्तन सबसे कम था, जो यह दर्शाता है कि यहाँ शहरीकरण की प्रक्रिया बहुत धीमी गति से हुई।
11. राजस्थान में, बाणगंगा का मेला कहां लगता है ?
राजस्थान में, बाणगंगा का मेला मैड़ (जयपुर) में लगता है।
यह मेला बैराठ (विराटनगर) तहसील के मैड़ नामक स्थान पर हर साल वैशाख पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन प्राचीन बाणगंगा नदी के किनारे किया जाता है, जिसका पौराणिक महत्व महाभारत काल से जुड़ा है। यह माना जाता है कि पांडवों के अज्ञातवास के दौरान, अर्जुन ने अपने बाण से इस नदी को उत्पन्न किया था।
यह मेला धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं।
12. गूदड़ सम्प्रदाय का प्रमुख पूजा स्थल (धाम) कहां स्थित है ?
गूदड़ संप्रदाय का प्रमुख पूजा स्थल (धाम) दांतड़ा, भीलवाड़ा में स्थित है।
गूदड़ संप्रदाय, संत रामदास जी द्वारा स्थापित एक वैष्णव संप्रदाय है। इस संप्रदाय के अनुयायी “गूदड़ी” (कपड़ों के टुकड़ों से बनी रजाई) पहनते हैं, जिसके कारण इसका नाम ‘गूदड़’ पड़ा। दांतड़ा में स्थित इनका प्रमुख धाम, उनके अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है।
13 प्रसिद्ध चित्रकार अली रजा, मुगल सेवा से मुक्त होकर राजस्थान में किस शासक के दरबार में शामिल हुए ?
प्रसिद्ध चित्रकार अली रजा मुगल सेवा से मुक्त होकर राजस्थान के अनूप सिंह के दरबार में शामिल हुए।
अनूप सिंह और बीकानेरी शैली
अली रजा का योगदान: अली रजा बीकानेर शैली के एक महत्वपूर्ण चित्रकार थे। वे मुगल बादशाह औरंगजेब की सेवा में थे, लेकिन उनकी कला की कद्र न होने के कारण वे अनूप सिंह के दरबार में चले आए।
उस्ता परिवार: अली रजा के साथ उनके बेटे भी बीकानेर आए, जिन्होंने मिलकर बीकानेरी चित्रकला की उस्ता शैली को विकसित किया। इस शैली में सोने के काम का विशेष महत्व है।
बीकानेर शैली का स्वर्ण युग: अनूप सिंह का शासनकाल (1669-1698) बीकानेर शैली का स्वर्ण युग माना जाता है। उन्होंने चित्रकारों को संरक्षण दिया और उन्हें अपने दरबार में प्रोत्साहित किया। अली रजा के साथ-साथ उनके पुत्र हसन रजा और रुक्नुद्दीन ने भी इस शैली को समृद्ध किया।
यह जानकारी हमें बीकानेर चित्रकला शैली के विकास में अनूप सिंह और चित्रकारों के योगदान को समझने में मदद करती है।
14. निम्नलिखित में से कौनसा / से सुषिर वाद्य यंत्र है / हैं?
सही उत्तर (3) A, B और C है। दिए गए सभी वाद्य यंत्र सुषिर वाद्य हैं।
सुषिर वाद्य यंत्र
सुषिर वाद्य उन वाद्य यंत्रों को कहते हैं, जिन्हें फूँक मारकर बजाया जाता है। ये यंत्र लकड़ी या धातु से बने होते हैं और इनमें हवा के प्रवाह से ध्वनि उत्पन्न होती है।
अलगोजा: यह दो बाँसुरी जैसा एक वाद्य यंत्र है, जिसे एक साथ मुँह से फूँक मारकर बजाया जाता है। यह राजस्थान का एक प्रमुख लोक वाद्य है और यहाँ के लोक संगीत में इसका विशेष स्थान है।
बांकिया: यह एक लंबा, तुरही जैसा वाद्य यंत्र है, जो धातु से बना होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से मांगलिक अवसरों और धार्मिक जुलूसों में किया जाता है।
सतारा: यह अलगोजा और शहनाई का एक मिश्रित रूप है। यह भी फूँक मारकर बजाया जाता है और इसका उपयोग अक्सर लोक संगीत में किया जाता है, खासकर पश्चिमी राजस्थान में।
इस प्रकार, ये तीनों ही वाद्य यंत्र हवा के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें सुषिर वाद्य की श्रेणी में रखा जाता है।
15. 1923 ई. में ब्यावरा से ‘राजस्थान’ नामक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन किसने आरंभ किया ?
1923 ई. में ब्यावर से ‘राजस्थान’ नामक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन ऋषि दत्त मेहता ने आरंभ किया था।
अखबार और स्वतंत्रता आंदोलन
‘राजस्थान’ अखबार का प्रकाशन उस समय शुरू हुआ जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। इस अखबार का उद्देश्य राजस्थान में राजनीतिक चेतना फैलाना और लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। ऋषि दत्त मेहता ने इस अखबार के माध्यम से ब्रिटिश सरकार की नीतियों और सामंती व्यवस्था की आलोचना की।
ऋषि दत्त मेहता: वे एक प्रमुख पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने राजस्थान में जन-जागृति लाने के लिए कई अखबारों का प्रकाशन किया।
ब्यावर: यह स्थान उस समय एक प्रमुख राजनीतिक केंद्र था और यहीं से कई राष्ट्रवादी गतिविधियों का संचालन होता था।
यह अखबार उस समय के महत्त्वपूर्ण आंदोलनों, जैसे किसान आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन, को समर्थन प्रदान करता था।
16. रक्षाबंधन के दिन बांधी गई राखियों को निम्नलिखित में से किस लोक देवता को अर्पित किया जाता है?
रक्षाबंधन के दिन बांधी गई राखियों को गोगाजी लोक देवता को अर्पित किया जाता है।
गोगाजी और राखी
रक्षाबंधन के बाद, जब इन राखियों का महत्व खत्म हो जाता है, तो उन्हें गोगाजी के थान (पूजा स्थल) पर जाकर चढ़ा दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गोगाजी, जिन्हें सर्प देवता के रूप में पूजा जाता है, इन राखियों को स्वीकार करते हैं। इस परंपरा के पीछे मान्यता यह है कि गोगाजी की पूजा करने से सर्प दंश से रक्षा होती है और यह एक शुभ कार्य माना जाता है।
17. निम्नलिखित में से कौनसा डिंगल शैली में इतिहास विषयक सामग्री का गद्य ग्रंथ नहीं है?
इनमें से झूलणा डिंगल शैली में इतिहास विषयक सामग्री का गद्य ग्रंथ नहीं है।
डिंगल साहित्य और उसकी शैलियाँ
डिंगल शैली पश्चिमी राजस्थान की एक साहित्यिक शैली है, जो चारण कवियों द्वारा विकसित की गई थी। इस शैली में कविता और गद्य दोनों शामिल हैं, जिनमें मुख्य रूप से वीर रस और ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन मिलता है।
विगत: यह एक प्रकार का गद्य ग्रंथ है जिसमें किसी राजवंश या व्यक्ति की पिछली घटनाओं, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का विस्तृत विवरण होता है। उदाहरण के लिए, “मारवाड़ रा परगना री विगत” (मुहणोत नैणसी द्वारा लिखित) एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक गद्य ग्रंथ है।
ख्यात: यह भी एक गद्य शैली है जिसमें किसी रियासत, राजवंश या व्यक्ति के इतिहास, वंशावली और उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया जाता है। “नैणसी री ख्यात” इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
वात: यह लोक कथाओं और ऐतिहासिक कहानियों का संग्रह है, जो अक्सर गद्य में लिखी जाती हैं। इनमें सामाजिक और नैतिक संदेश भी निहित होते हैं।
झूलणा: यह एक काव्य शैली है, न कि गद्य ग्रंथ। यह एक प्रकार का छंद है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति की प्रशंसा में कविताएँ लिखने के लिए किया जाता है। इसमें वीर रस का प्रमुखता से उपयोग होता है। इसका विषय ऐतिहासिक हो सकता है, लेकिन इसका रूप गद्य नहीं बल्कि पद्य (काव्य) होता है।
इस प्रकार, विगत, ख्यात और वात गद्य ग्रंथ हैं, जबकि झूलणा एक काव्य विधा है।
18. औरंगजेब ने महाराणा राजसिंह को कौनसे परगने प्रदान किए थे ?
19. ‘नेवरी’ आभूषण स्त्रियां कहां पहनती हैं ?
‘नेवरी’ आभूषण स्त्रियाँ पैर में पहनती हैं।
यह राजस्थान में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला एक पारंपरिक आभूषण है, जिसे पैरों में पहना जाता है। यह एक प्रकार की मोटी पायल होती है, जो अक्सर चाँदी से बनी होती है और इसमें घुँघरू भी लगे होते हैं। इसे पहनने पर चलने से मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है, जो राजस्थानी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है।
20. निम्नलिखित में से राजस्थान के किस किले पर कभी बाहरी आक्रमण नहीं हुआ ?
21. दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति का विकास हुआ ?
दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में आहड़ नामक प्राचीन संस्कृति का विकास हुआ।
आहड़ सभ्यता
आहड़ सभ्यता, जिसे ताम्रयुगीन सभ्यता के रूप में जाना जाता है, राजस्थान के उदयपुर जिले में बनास नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई थी। यह सभ्यता लगभग 4000 वर्ष पुरानी मानी जाती है।स्थल: आहड़ के प्रमुख स्थल उदयपुर के निकट आहड़, गिलूंड, बालाथल आदि हैं। ये स्थल बनास नदी बेसिन में स्थित हैं, इसलिए इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है।
विशेषताएँ:
तांबे के औजार: यहाँ तांबे के औजार, बर्तन और आभूषण बड़ी मात्रा में मिले हैं, जो यह दर्शाते हैं कि यहाँ के लोग तांबे का उपयोग जानते थे। इसी कारण इसे “ताम्रवती नगरी” भी कहा जाता है।
पक्की ईंटों का उपयोग: यहाँ के निवासी पक्की ईंटों से घर बनाते थे, जो उस समय के लिए एक उन्नत तकनीक थी।
कृषि और पशुपालन: यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन दोनों का काम करते थे।
व्यापार: अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापारिक संबंध भी थे।
अन्य संस्कृतियाँ
कालीबंगा: यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और यह एक हड़प्पाकालीन सभ्यता थी।
गणेश्वर: यह सीकर जिले में स्थित है और इसे “ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी” कहा जाता है।
बैराठ: यह जयपुर जिले में स्थित है और यह महाभारतकालीन और मौर्यकालीन संस्कृति से संबंधित है।
इस प्रकार, भौगोलिक रूप से, आहड़ सभ्यता दक्षिण-पूर्वी राजस्थान से संबंधित है।
22. ‘पाग-दस्तूर किसे कहा जाता है ?
‘पाग-दस्तूर’ परिवार में मुखिया की मृत्यु के बाद निश्चित दिन पर होने वाला दस्तूर था।
यह एक प्रकार की उत्तराधिकार प्रथा है, जिसमें परिवार के सबसे बड़े बेटे या योग्य सदस्य को पगड़ी पहनाकर मुखिया की जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। इस परंपरा को पगड़ी रस्म भी कहा जाता है।
पाग-दस्तूर का महत्व
उत्तराधिकार का प्रतीक: यह रस्म परिवार की मुखिया के पद के औपचारिक हस्तांतरण का प्रतीक है।
सामाजिक मान्यता: इस रस्म के माध्यम से समुदाय और परिवार के सदस्यों के सामने नए मुखिया को स्वीकार किया जाता था।
पारिवारिक जिम्मेदारी: पगड़ी पहनाना इस बात का प्रतीक है कि अब नए मुखिया पर परिवार की सभी जिम्मेदारियाँ आ गई हैं।
यह रस्म आज भी कई ग्रामीण और पारंपरिक परिवारों में निभाई जाती है।
23. निम्नलिखित में से झालावाड़ के किस शासक को तात्या टोपे ने गिरफ्तार किया था ?
झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह को तात्या टोपे ने गिरफ्तार किया था।
तात्या टोपे और झालावाड़ का संघर्ष
1857 के विद्रोह के दौरान, तात्या टोपे ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। जब वे राजस्थान पहुँचे, तो वे झालावाड़ रियासत में भी गए।
तात्या का झालावाड़ में प्रवेश: तात्या टोपे 1858 में झालावाड़ पहुँचे। उन्होंने वहाँ के शासक पृथ्वी सिंह से अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता माँगी।
पृथ्वी सिंह का रुख: पृथ्वी सिंह ने अंग्रेजों के साथ अपनी निष्ठा बनाए रखी और तात्या टोपे की सहायता करने से इनकार कर दिया।
तात्या द्वारा घेराव: पृथ्वी सिंह के इस रुख से नाराज होकर, तात्या टोपे ने झालावाड़ के किले का घेराव कर लिया और राजा को समर्पण करने पर मजबूर किया।
गिरफ्तारी और फिरौती: तात्या टोपे ने पृथ्वी सिंह को गिरफ्तार कर लिया और उनसे भारी मात्रा में धन, तोपें और हथियार प्राप्त किए। यह घटना 1857 के विद्रोह में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जहाँ एक क्रांतिकारी ने एक रियासत के शासक को सीधे चुनौती दी।
यह घटना झालावाड़ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है और यह दर्शाती है कि कैसे 1857 के विद्रोह ने रियासतों और ब्रिटिश सत्ता के बीच संबंधों को प्रभावित किया।
24. निम्नलिखित में से कौनसा / से कथन सही है हैं?
दिए गए कथनों में से, सभी A, B और C सही हैं।
बैराठ सभ्यता और उत्खनन
बैराठ (प्राचीन विराटनगर), जयपुर जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, जो महाभारत और मौर्य काल से संबंधित है।
कथन (A): के.एन. दीक्षित बैराठ में उत्खनन से संबंधित हैं। दयाराम साहनी द्वारा 1936-37 में किए गए प्रारंभिक उत्खनन के बाद, 1962-63 में कैलाश नाथ दीक्षित ने इस स्थल पर उत्खनन का कार्य जारी रखा, जिससे और भी महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए।
कथन (B): बैराठ से सूती वस्त्र का एक टुकड़ा प्राप्त हुआ था। यह उत्खनन में मिला एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य है, जो यह दर्शाता है कि यहाँ के लोग वस्त्र निर्माण और बुनाई से परिचित थे।
कथन (C): बैराठ में बीजक की पहाड़ी पर एक अशोक-कालीन वृत्ताकार मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। दयाराम साहनी ने अपनी रिपोर्ट में इस मंदिर का विशेष रूप से उल्लेख किया था। यह मंदिर ईंटों से बना था और इसमें लकड़ी के खंभे लगे हुए थे। यह साक्ष्य बैराठ के मौर्यकालीन महत्व को स्थापित करता है, जहाँ बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था। यहाँ पर मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित एक शिलालेख भी मिला है, जिसे भाब्रू शिलालेख के नाम से जाना जाता है।
इस प्रकार, ये तीनों ही कथन बैराठ सभ्यता के बारे में सही जानकारी देते हैं।
25. राम प्यारी बेन हेजा बेन एवं रुक्मणी बेन आदि महिलाओं ने 1939 ई. में किस रियासत के प्रजामण्डल आंदोलन में भाग लिया था?
राम प्यारी बेन, हेजा बेन और रुक्मणी बेन जैसी महिलाओं ने 1939 ई. में सिरोही रियासत के प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया था।
सिरोही प्रजामंडल आंदोलन
स्थापना: सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में मुंबई में हुई थी, जिसका उद्देश्य सिरोही रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था।
प्रमुख महिला नेता: इस आंदोलन में कई महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया, जिनमें राम प्यारी बेन, हेजा बेन और रुक्मणी बेन प्रमुख थीं। उन्होंने महिलाओं को संगठित करने, राजनीतिक जागरूकता फैलाने और सत्याग्रह में भाग लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
आंदोलन का स्वरूप: यह आंदोलन रियासती शासन के दमनकारी कानूनों और ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ था। इन महिलाओं के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों और सभाओं ने आंदोलन को और भी मजबूत बनाया।
इन महिलाओं का योगदान यह दर्शाता है कि राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलनों में पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं ने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया और स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
26. सल्तनत काल के दो मूल सिक्के चांदी का टांका और तांबे का जीटल किसने प्रचलित किए ?
सल्तनत काल में चांदी का टांका और तांबे का जीतल सिक्के इल्तुतमिश ने प्रचलित किए थे।
इल्तुतमिश का योगदान
इल्तुतमिश (1211-1236 ईस्वी) दिल्ली सल्तनत का एक प्रमुख शासक था, जिसने सल्तनत की प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था को मजबूत किया। उसने मुद्रा प्रणाली में सुधार लाने के लिए ये दो महत्वपूर्ण सिक्के चलाए:
टांका: यह शुद्ध चांदी का सिक्का था, जिसका वजन लगभग 175 ग्रेन (लगभग 11.3 ग्राम) था। यह सल्तनत काल में मानक मुद्रा बन गया।
जीतल: यह तांबे का सिक्का था और इसका उपयोग छोटी लेन-देन के लिए किया जाता था। टांका और जीतल के बीच एक निश्चित अनुपात था, जिससे मुद्रा विनिमय आसान हो गया।
इल्तुतमिश के इन सुधारों ने सल्तनत की अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान की और उसके शासन को एक मजबूत आधार दिया।
27. भील विद्रोह के संबंध में कौनसा / से कथन सत्य है/हैं?
दिए गए सभी कथन (a), (b) और (c) भील विद्रोह के संबंध में सत्य हैं। सही कूट (2) A, B एवं C है।
भील विद्रोह के कारण
भील विद्रोह, जो 19वीं सदी की शुरुआत में राजस्थान और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में हुआ था, कई जटिल कारकों का परिणाम था:
स्वतःस्फूर्त प्रकृति (a): भील विद्रोह प्रारंभिक चरण में किसी सुनियोजित नेतृत्व के बजाय स्थानीय और तात्कालिक कारणों से हुआ था। जब अंग्रेजों ने भीलों के पारंपरिक अधिकारों में हस्तक्षेप करना शुरू किया, तो उन्होंने स्वतःस्फूर्त रूप से इसका विरोध किया।
नई व्यवस्था की प्रतिक्रिया (b): अंग्रेजों ने अपने शासन को स्थापित करने के लिए भीलों के पारंपरिक अधिकारों, जैसे वन उत्पादों पर उनके अधिकार और उनके स्थानीय प्रशासन, में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इस नई व्यवस्था ने उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन को प्रभावित किया, जिससे विद्रोह शुरू हो गया।
बाह्य तत्वों का प्रवेश (c): अंग्रेजों ने भीलों के क्षेत्र में नए अधिकारियों और व्यापारियों को नियुक्त किया, जिन्हें भीलों की संस्कृति और जीवनशैली की समझ नहीं थी। इन बाहरी तत्वों के प्रवेश से सामाजिक तनाव उत्पन्न हुआ और भीलों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हथियार उठा लिए।
ये तीनों कारक मिलकर भील विद्रोह के लिए जिम्मेदार थे, जो उनकी पारंपरिक जीवनशैली पर हो रहे हमलों की प्रतिक्रिया थी।
28. चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय द्वारा भण्डानकों के दमन का उल्लेख किस तत्कालीन विद्वान ने अपनी कविता में किया है ?
29. किन दो क्षेत्रों को विलय, 1956 ईस्वी में, राज्य पुनर्गठन आयोग एवं मुनी जिनविजय समिति की सिफारिश पर राजस्थान में किया गया ?
राज्य पुनर्गठन आयोग और मुनि जिनविजय समिति की सिफारिश पर, 1956 में आबू रोड – देलवाड़ा क्षेत्र का विलय राजस्थान में किया गया।
एकीकरण का अंतिम चरण
राजस्थान का एकीकरण कुल सात चरणों में पूरा हुआ। इसका सातवां और अंतिम चरण 1 नवंबर 1956 को संपन्न हुआ। इसी दौरान, भारत सरकार द्वारा नियुक्त राज्य पुनर्गठन आयोग (जिसके अध्यक्ष फजल अली थे) और मुनि जिनविजय समिति की सिफारिशों को लागू किया गया।
आबू रोड – देलवाड़ा का विलय: सिरोही रियासत के ये क्षेत्र गुजरात के साथ मिलाए जाने थे। लेकिन राजस्थान की जनता, विशेषकर गोकुल भाई भट्ट के नेतृत्व में, इन क्षेत्रों को राजस्थान में शामिल करने के लिए लगातार आंदोलन चला रही थी।
सिरोंज का स्थानांतरण: इसी चरण में, राजस्थान के झालावाड़ जिले का सिरोंज उपखंड मध्य प्रदेश को दिया गया।
सुनेल टप्पा का विलय: मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के सुनेल टप्पा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया।
अजमेर-मेरवाड़ा का विलय: इस चरण में अजमेर-मेरवाड़ा (जो एक केंद्र शासित प्रदेश था) को भी राजस्थान में शामिल कर लिया गया।
इस प्रकार, आबू रोड और देलवाड़ा का विलय राजस्थान के एकीकरण में एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने राजस्थान को उसका वर्तमान स्वरूप दिया।
30. प्रतिहारों के शासन काल में किस स्थापत्य शैली का विकास हुआ ?
प्रतिहारों के शासनकाल में महामारू स्थापत्य शैली का विकास हुआ।
महामारू शैली की विशेषताएँ
महामारू शैली, जिसे गुर्जर-प्रतिहार शैली भी कहते हैं, आठवीं से दसवीं शताब्दी के बीच विकसित हुई थी। यह शैली मुख्य रूप से मंदिरों के निर्माण से संबंधित है और यह अपनी विशिष्ट विशेषताओं के लिए जानी जाती है:
शिखर: इस शैली के मंदिरों में ऊंचे और जटिल शिखर होते हैं, जो एक-दूसरे को काटती हुई रेखाओं से बने होते हैं।
गर्भगृह: गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा और गोलाकार शिखर होता है।
जटिल नक्काशी: मंदिरों की दीवारों पर देवी-देवताओं, युद्ध के दृश्यों और अन्य पौराणिक कथाओं की जटिल नक्काशी होती है।
उदाहरण: इस शैली के प्रमुख उदाहरणों में ओसिया (जोधपुर) में स्थित मंदिर, किराडू के मंदिर (बाड़मेर) और अम्बिका माता मंदिर (जगत, उदयपुर) शामिल हैं।
यह शैली उस समय की स्थापत्य कला में एक महत्वपूर्ण विकास का प्रतिनिधित्व करती है और इसने बाद में आने वाली कई अन्य शैलियों को प्रभावित किया।
31. राष्ट्रपति निर्वाचन 2022 में, राजस्थान राज्य विधानसभा के सभी सदस्यों का कुल मत-मूल्य कितना था ?
राष्ट्रपति निर्वाचन 2022 में, राजस्थान राज्य विधानसभा के सभी सदस्यों का कुल मत-मूल्य 25800 था।
मत-मूल्य की गणना
राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्येक विधायक के मत का एक निश्चित मूल्य होता है। इस मूल्य की गणना एक विशेष सूत्र से की जाती है:
राजस्थान में विधायक: राजस्थान विधानसभा में कुल 200 विधायक हैं।
1971 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या: राजस्थान की जनसंख्या 2,57,65,809 थी।
उपर्युक्त सूत्र के अनुसार, राजस्थान के प्रत्येक विधायक के मत का मूल्य:
इसलिए, एक विधायक के मत का मूल्य 129 था।
अब, कुल मत-मूल्य की गणना इस प्रकार की जाएगी:
अतः, 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान के सभी विधायकों का कुल मत-मूल्य 25800 था।
32. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार पंचायत समिति के उप-प्रधान की शक्तियों और कार्यों के संबंध में गलत कथन की पहचान करें
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार, पंचायत समिति के उप-प्रधान की शक्तियों और कार्यों के संबंध में गलत कथन है:
(3) उप-प्रधान, प्रधान की शक्तियों और कार्यो का प्रयोग कर सकता है, यदि प्रधान 30 दिन से अधिक अवधि के लिए पंचायत समिति क्षेत्र से अनुपस्थित रहता है।
सही व्याख्या
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 46 के अनुसार, उप-प्रधान की शक्तियों और कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जिसके आधार पर सही कथन इस प्रकार हैं:
प्रधान की अनुपस्थिति में शक्तियाँ: उप-प्रधान प्रधान की शक्तियों का उपयोग कर सकता है और उसके कर्तव्यों का पालन कर सकता है यदि प्रधान 60 दिनों से अधिक समय तक पंचायत समिति के क्षेत्र से अनुपस्थित रहता है। यह प्रधान के चुनाव लंबित होने की स्थिति में भी लागू होता है। अतः, विकल्प (1) सही है।
बैठकों की अध्यक्षता: यदि प्रधान किसी बैठक में अनुपस्थित है, तो उप-प्रधान उस बैठक की अध्यक्षता करता है। अतः, विकल्प (2) सही है।
प्रधान द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ: उप-प्रधान को प्रधान द्वारा लिखित आदेश के माध्यम से ऐसी शक्तियाँ और कर्तव्य सौंपे जा सकते हैं जो सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन हों। अतः, विकल्प (4) सही है।
चूंकि अधिनियम में प्रधान की अनुपस्थिति की अवधि 60 दिन बताई गई है, न कि 30 दिन, इसलिए विकल्प (3) गलत है। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि प्रधान की अनुपस्थिति में भी पंचायत समिति का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे।
33. भारत के संविधान के किस प्रावधान के तहत, राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत किसी व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों से संबंधित राजस्थान Feb लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनिवार्य हैं?
भारत के संविधान के अनुच्छेद 320(3) के तहत, राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत किसी व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों से संबंधित राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) से परामर्श करना अनिवार्य है।
अनुच्छेद 320(3) का प्रावधान
यह अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और राज्य लोक सेवा आयोगों (SPSC) के कार्यों से संबंधित है। इसके खंड (3) में कुछ विशिष्ट मामलों का उल्लेख है, जिनमें आयोग से परामर्श करना अनिवार्य होता है। इनमें से एक प्रावधान यह है कि अनुशासनात्मक मामलों में आयोग से परामर्श किया जाएगा।
अनुशासनिक मामले: इसका अर्थ है किसी भी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध की जाने वाली अनुशासनात्मक कार्रवाई, जैसे कि बर्खास्तगी, सेवा से हटाया जाना, पद में अवनति, या अन्य कोई दंड।
परामर्श का उद्देश्य: यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी कर्मचारियों के मामलों में निष्पक्षता और न्याय बनी रहे। लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, और इसका परामर्श अनुशासनात्मक कार्रवाई को राजनीतिक दबाव से मुक्त रखने में मदद करता है।
अनुच्छेद 311 से संबंध: हालांकि अनुच्छेद 311 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्तगी, हटाने या पद में अवनति से सुरक्षा प्रदान करता है, अनुच्छेद 320(3) यह सुनिश्चित करता है कि ऐसी किसी भी कार्रवाई से पहले आयोग से परामर्श लिया जाए, जिससे अनुच्छेद 311 के प्रावधानों को मजबूती मिलती है।
इसलिए, अनुशासनात्मक मामलों में RPSC से परामर्श करना एक संवैधानिक अनिवार्यता है, जो अनुच्छेद 320(3) के तहत निर्धारित है।
34. निम्नलिखित में से किस विषय पर, राजस्थान विधानसभा कोई कानून नहीं बना सकती है ?
राजस्थान विधानसभा निगम कर (Corporation Tax) पर कोई कानून नहीं बना सकती है।
संवैधानिक शक्तियाँ
भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसमें तीन सूचियाँ हैं:
संघ सूची (Union List): इस सूची में वर्णित विषयों पर केवल संसद कानून बना सकती है।
राज्य सूची (State List): इस सूची में वर्णित विषयों पर केवल राज्य विधानसभा कानून बना सकती है।
समवर्ती सूची (Concurrent List): इस सूची में वर्णित विषयों पर संसद और राज्य विधानसभा दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन यदि किसी विषय पर दोनों के कानून में टकराव होता है, तो संसद का कानून मान्य होगा।
निगम कर संघ सूची का विषय है (प्रविष्टि 85)। इसलिए, इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल भारत की संसद के पास है।
इसके विपरीत, कृषि आय पर कर, वृत्तियों (professions) पर कर और पथ कर (road tax) राज्य सूची के विषय हैं, और इन पर कानून बनाने का अधिकार राजस्थान विधानसभा को प्राप्त है।
35. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण या प्राक्कलित आय और व्यय का विवरण राजस्थान विधानसभा में ऐसे दिन उपस्थापित किया जाता है, जो निर्धारित की जाती है –
प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण या प्राक्कलित आय और व्यय का विवरण राजस्थान विधानसभा में ऐसे दिन उपस्थापित किया जाता है, जो राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती है।
वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 में राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण (जिसे सामान्यतः राज्य का बजट कहा जाता है) का प्रावधान है। इस अनुच्छेद के अनुसार:
राज्यपाल की भूमिका: राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानमंडल (राजस्थान के मामले में विधानसभा) के समक्ष राज्य के प्राक्कलित आय और व्यय का विवरण प्रस्तुत करवाता है।
बजट प्रस्तुत करने की तिथि: हालांकि, बजट प्रस्तुत करने की तिथि का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्यपाल राज्य सरकार, विशेषकर मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के साथ परामर्श करके यह तिथि तय करते हैं।
संवैधानिक प्रक्रिया: यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके तहत राज्य सरकार की वित्तीय योजनाएं और नीतियां विधानमंडल के सामने रखी जाती हैं, ताकि उन पर चर्चा और अनुमोदन किया जा सके।
इस प्रकार, बजट प्रस्तुत करने की तिथि तय करने का अधिकार राज्यपाल के पास है।
36. राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किस ने प्रथम बार राजस्थान विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया ?
राजस्थान विधानसभा में प्रथम बार बजट प्रस्तुत करने वाले मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे।
टीकाराम पालीवाल राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 3 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1952 तक इस पद पर कार्य किया। उनके कार्यकाल में ही राजस्थान का पहला विधानसभा बजट प्रस्तुत किया गया था।
37. 31 मई 2025 को यथाविद्यमान राजस्थान मंत्रिपरिषद् के संबंध में निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही नहीं हैं ?
31 मई 2025 को यथाविद्यमान राजस्थान मंत्रिपरिषद् के संबंध में निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही नहीं है, यह जानने के लिए हमें उस समय की वास्तविक स्थिति को देखना होगा।
राजस्थान के वर्तमान मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित कुल 24 सदस्य हैं।
31 मई 2025 तक, राजस्थान मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित कुल 24 सदस्य थे। यह कथन सही है।
राजस्थान के वर्तमान मंत्रिपरिषद् में 06 और मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है।
राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 200 है। संविधान के 91वें संशोधन अधिनियम, 2003 के अनुसार, किसी भी राज्य में मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या, मुख्यमंत्री सहित, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती।
200 का 15% = 30।
इसका मतलब है कि राजस्थान में अधिकतम 30 मंत्री (मुख्यमंत्री सहित) हो सकते हैं।
31 मई 2025 को, मंत्रिपरिषद में 24 सदस्य थे, इसलिए 30-24 = 6 और मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती थी। यह कथन भी सही है।
वर्तमान राजस्थान मंत्रिपरिषद् में दो महिला सदस्य हैं।
31 मई 2025 तक, राजस्थान मंत्रिपरिषद में दो महिला सदस्य (दिया कुमारी और मंजू बाघमार) थीं। यह कथन भी सही है।
वर्तमान मंत्रिपरिषद् में कुल 10 राज्यमंत्री हैं, जिनमें से 05 राज्य मंत्रियों के पास स्वतंत्र प्रभार है।
31 मई 2025 को, राजस्थान मंत्रिपरिषद में कुल 12 राज्यमंत्री थे। इनमें से 5 राज्यमंत्रियों के पास स्वतंत्र प्रभार था, जबकि 7 राज्यमंत्री के पास स्वतंत्र प्रभार नहीं था।
इसलिए, यह कथन कि कुल 10 राज्यमंत्री थे, सही नहीं है।
अतः, विकल्प (4) सही नहीं है।
38. निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के सबसे लंबे समय तक मुख्य सचिव रहे हैं ?
राजस्थान के सबसे लंबे समय तक मुख्य सचिव रहने वाले व्यक्ति श्री एम.एल. मेहता हैं। उन्होंने 14 अप्रैल 1994 से 30 नवंबर 1997 तक इस पद पर अपनी सेवाएं दीं, जो कि लगभग 3 साल, 7 महीने और 16 दिन है।
एम.एल. मेहता: एक संक्षिप्त परिचय
एम.एल. मेहता (मोतीलाल मेहता) भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के एक अधिकारी थे, जिन्होंने राजस्थान में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। उन्हें विशेष रूप से राजस्थान के सबसे लंबे समय तक मुख्य सचिव के रूप में जाना जाता है।
मुख्य सचिव के रूप में कार्यकाल
श्री मेहता ने 14 अप्रैल 1994 से 30 नवंबर 1997 तक राजस्थान के मुख्य सचिव का पद संभाला। यह कार्यकाल लगभग 3 साल, 7 महीने और 16 दिन का था, जो कि अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल है।
अन्य महत्वपूर्ण पद और उपलब्धियाँ
प्रमुख शासन सचिव: मुख्य सचिव बनने से पहले उन्होंने विभिन्न विभागों में प्रमुख शासन सचिव के रूप में कार्य किया।
प्रशासनिक सुधारों में योगदान: उन्हें राज्य के प्रशासन में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए कई सुधारों का श्रेय दिया जाता है।
लेखन: उन्होंने अपने अनुभवों और प्रशासनिक विषयों पर कई लेख और पुस्तकें भी लिखीं।
श्री मेहता को राजस्थान के प्रशासनिक इतिहास में एक प्रभावी और ईमानदार अधिकारी के रूप में याद किया जाता है।
39. भारत के संविधान में राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित अनुच्छेदों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए –
उपर्युक्त युग्मों में से, केवल III और IV सही हैं।
आइए प्रत्येक अनुच्छेद को विस्तार से समझते हैं:
राज्यपाल की शक्तियां और संबंधित अनुच्छेद
I. क्षमा दान की राज्यपाल की शक्ति – अनुच्छेद 162: यह युग्म गलत है। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 161 में है, न कि 162 में। अनुच्छेद 162 का संबंध राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से है।
II. अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति – अनुच्छेद 214: यह युग्म भी गलत है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 के तहत प्राप्त है। अनुच्छेद 214 का संबंध राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों के गठन से है।
III. विधेयकों पर अनुमति – अनुच्छेद 200: यह युग्म सही है। अनुच्छेद 200 राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी सहमति देने, उसे रोकने या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने की शक्ति प्रदान करता है।
IV. राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन – अनुच्छेद 174: यह युग्म सही है। अनुच्छेद 174 राज्यपाल को समय-समय पर राज्य विधानमंडल के सदनों (या सदन) को आहूत करने, सत्रावसान करने और विधानसभा को भंग करने का अधिकार देता है।
इस प्रकार, केवल युग्म III और IV सही हैं, जो विकल्प (4) में दिया गया है।
40. निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के एक अध्यक्ष नहीं थे ?
राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों की सूची :
न्यायमूर्ति कांता भटनागर (प्रथम अध्यक्ष)
न्यायमूर्ति सैय्यद सगीर अहमद
न्यायमूर्ति प्रकाश चंद्र जैन (कार्यवाहक अध्यक्ष)
न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन
न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास (वर्तमान अध्यक्ष)
दिए गए विकल्पों में से, न्यायमूर्ति प्रेमचंद जैन इस आयोग के अध्यक्ष नहीं थे। इसलिए, सही उत्तर न्यायमूर्ति प्रेमचंद जैन है।
41. राजस्थानी भाषा के लिये किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हेतु चयनित किया गया है ?
- विजेता: पूनम चंद गोदारा
- भाषा: राजस्थानी
- पुस्तक: अंतस रै आंगणै
- वर्ष: 2025
42. 24 जुलाई 2025 तक आभा आईडी बनाने में राजस्थान का देश में स्थान है –
- दूसरा स्थान:आभा आईडी बनाने के मामले में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है.
- आभा आईडी की संख्या:प्रदेश में 6 करोड़ से अधिक आभा आईडी बनाई जा चुकी हैं.
- लक्ष्य:प्रदेश में लोगों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए ये आईडी बनाई जा रही हैं.
43. जुलाई 2025 में चीन में आयोजित 11 वीं एशियाई महिला युवा हँडबॉल चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए –
जुलाई 2025 में चीन में आयोजित होने वाली 11वीं एशियाई महिला युवा हैंडबॉल चैंपियनशिप के बारे में दिए गए दोनों कथन असत्य हैं।
निष्कर्ष का कारण
यह प्रतियोगिता अभी तक आयोजित नहीं हुई है। 11वीं एशियाई महिला युवा हैंडबॉल चैंपियनशिप जुलाई 2025 में चीन में प्रस्तावित है, लेकिन इसके लिए भारतीय टीम का चयन और कोच की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। किसी भी खेल प्रतियोगिता के लिए टीम का चयन और कोचिंग स्टाफ का निर्धारण आमतौर पर इवेंट से कुछ ही समय पहले होता है। चूँकि यह इवेंट भविष्य में है, इसलिए कथन A और B में दी गई जानकारी की पुष्टि नहीं की जा सकती है और इसलिए वे गलत हैं।
सही विकल्प है: (1) कथन A और B दोनों असत्य है।
44. जुलाई 2025 में, राजस्थान के मंत्रिमंडल ने गेल (इंडिया) लिमिटेड और आरवीयूएनएल के मध्य ज्वॉइंट वेंचर कंपनी के गठन की मंजदूरी दी है। इसके संदर्भ में निम्न में से कौनसा कथन सही नहीं है?
- संयुक्त उद्यम समझौते के अनुसार, धौलपुर गैस आधारित पॉवर प्लांट की 530 मेगावाट क्षमता की नहीं, बल्कि 330 मेगावाट क्षमता की मौजूदा इकाई हस्तांतरित की जाएगी।
- संयुक्त उद्यम में गेल और आरवीयूएनएल के बीच इक्विटी निवेश के माध्यम से समान भागीदारी होगी, जिससे शेयरधारिता 50-50% होगी।
- संयुक्त उद्यम कंपनी रामगढ़ में 270.5 मेगावाट की गैस-आधारित इकाई और धौलपुर में 330 मेगावाट की गैस-आधारित इकाई हस्तांतरित करेगी। इसके अतिरिक्त, यह 750 मेगावाट की सौर ऊर्जा और 250 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना भी करेगी।
45. राजस्थान के पहलवानों द्वारा क्रमशः स्वर्ण, रजत व कांस्य पदकों का सही संयोजन चुनें, जो उनके द्वारा बिहार में आयोजित खेलों इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कुश्ती में जीते गए
- (1) स्वर्ण – 1, रजत 2, कांस्य -6:गलत है, क्योंकि यह संयोजन सही नहीं है।
- (2) स्वर्ण – 3, रजत – 2, कांस्य 5:गलत है, क्योंकि यह संयोजन सही नहीं है।
- (3) स्वर्ण – 2, रजत 1, कांस्य – 6:यह संयोजन सही है, क्योंकि राजस्थान के पहलवानों ने कुश्ती में कुल 9 पदक जीते थे, जिसमें 2 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल थे।
- (4) स्वर्ण – 2, रजत – 3, कांस्य 5:गलत है, क्योंकि यह संयोजन सही नहीं है।
46. जुलाई, 2025 में, देश का पहला राजकीय बालिका सैनिक विद्यालय किस जिले में, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री द्वारा उद्घाटित किया गया ?
47. राजस्थान के मंत्रिमंडल द्वारा जुलाई 2025 में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पॉलिसी (हील इन राजस्थान नीति 2025) के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। इसके अनुसार इस नीति के क्रियान्वयन हेतु गठित होने वाली तकनीकी समिति के अध्यक्ष होंगे
राजस्थान के मंत्रिमंडल द्वारा जुलाई 2025 में अनुमोदित मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पॉलिसी (हील इन राजस्थान नीति 2025) के क्रियान्वयन हेतु गठित होने वाली तकनीकी समिति के अध्यक्ष मेडिकल शिक्षा सचिव होंगे।
48. उन गांवों का सही संयोजन चुनें जिनके नाम जून 2025 में रामसर साइट में जोड़े गए हैं
जून 2025 में रामसर साइट्स में जोड़े गए गांवों का सही संयोजन (A) मेनार और (C) खीचन है।
सही विकल्प है: (3) A और C
प्रमुख जानकारी
मेनार (उदयपुर): इसे ‘बर्ड विलेज’ के नाम से जाना जाता है और यह एक महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि क्षेत्र है जो विभिन्न प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करता है।
खीचन (जोधपुर): यह गांव विशेष रूप से कुर्जां (डेमोइसेल क्रेन) के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल हजारों की संख्या में ये पक्षी प्रवास के लिए आते हैं, जिससे यह एक महत्वपूर्ण पक्षी अभयारण्य बन गया है।
केवलादेव पहले से ही एक रामसर साइट (1981 से) है, इसलिए इसे ‘जोड़ा गया’ नहीं कहा जा सकता। गजनेर को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है।
49. जून 2025 में, राजस्थान के किस शहर में, पोंटून तकनीक से बनी राज्य की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बोट का शुभारंभ किया गया हैं?
सही उत्तर है उदयपुर।
जून 2025 में, राजस्थान के उदयपुर शहर में पोंटून तकनीक से बनी राज्य की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बोट का शुभारंभ किया गया है।
50. जुलाई 2025 में, राजस्थान क्रिकेट संघ की तदर्थ समिति ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली टीम चुनने के लिए चयन समिति की घोषणा की। निम्नलिखित में से कौन सीनियर पुरूष वर्ग की चयन समिति में शामिल नहीं हैं?
दिए गए विकल्पों में से, नरेश गहलोत सीनियर पुरूष वर्ग की चयन समिति में शामिल नहीं हैं।
विवरण
जुलाई 2025 में, राजस्थान क्रिकेट संघ (RCA) की तदर्थ समिति द्वारा घोषित सीनियर पुरूष चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:
अध्यक्ष: विलास जोशी
सदस्य: राहुल कांवट
सदस्य: कुलदीप सिंह
नरेश गहलोत को अंडर-19 चयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, न कि सीनियर पुरूष चयन समिति का।
51. माटो ग्रोसो पठार किस महाद्वीप में स्थित है ?
माटो ग्रोसो पठार दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है।
यह पठार मुख्य रूप से ब्राजील में स्थित है, और इसका नाम ब्राजील के माटो ग्रोसो राज्य पर रखा गया है। यह पठार अमेज़ॅन बेसिन और पराग्वे नदी बेसिन के बीच एक जल-विभाजन का काम करता है।
- यह ब्राज़ीलियाई हाइलैंड्स का एक प्राचीन, अपरदित (इरोड किया हुआ) पठार है।
- यह अधिकांश माटो ग्रोसो राज्य में फैला हुआ है।
- यह पठार उत्तर में अमेज़ॅन नदी बेसिन और दक्षिण में पराग्वे नदी बेसिन के बीच एक जल विभाजक के रूप में काम करता है।
- इस क्षेत्र में मुख्यतः सवाना घास के मैदान और जंगल (सेराडो) का मिश्रण पाया जाता है।
- इसका औसत उन्नयन लगभग 3,000 फीट (900 मीटर) है।
- पठार के दक्षिणी भाग में पैंटानल नामक बाढ़ के मैदान हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय वेटलैंड्स में से एक हैं।
- इस क्षेत्र की प्राथमिक आर्थिक गतिविधि पशुपालन है, हालांकि यहाँ खनन भी किया जाता है।
- यह पठार अपने समृद्ध इतिहास और विविध पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जाना जाता है।
52. वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिसम्बर, 2024 तक) भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ ?
- FY 2024-25 में महाराष्ट्र को $16.651 बिलियन का FDI प्राप्त हुआ, जो भारत के कुल FDI इक्विटी प्रवाह का 31% है।
- इस अवधि के दौरान, कर्नाटक $4.496 बिलियन FDI इक्विटी प्रवाह के साथ दूसरे स्थान पर रहा।
53. भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा की परिवर्तिता 20% से कम हैं?
उत्तरी-पूर्वी राज्यों में वार्षिक वर्षा की परिवर्तिता 20% से कम है।
विवरण
वार्षिक वर्षा की परिवर्तिता से तात्पर्य वर्ष-दर-वर्ष वर्षा की मात्रा में होने वाले उतार-चढ़ाव से है। इसे प्रतिशत में मापा जाता है।
कम परिवर्तिता (<20%): जिन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा की मात्रा अधिक और विश्वसनीय होती है, वहाँ परिवर्तिता कम होती है। भारत के उत्तर-पूर्वी राज्य, पश्चिमी तट, और गंगा के मैदानी इलाकों में भारी वर्षा होती है, इसलिए यहाँ परिवर्तिता कम है।
मध्यम परिवर्तिता (20% – 50%): यह परिवर्तिता गंगा के मैदान के कुछ हिस्सों और ओडिशा, झारखंड, बिहार, पूर्वी तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में पाई जाती है।
उच्च परिवर्तिता (>50%): कम वर्षा वाले क्षेत्रों में परिवर्तिता अधिक होती है। उदाहरण के लिए, राजस्थान के पश्चिमी हिस्से, गुजरात, और दक्कन के पठार के कुछ भाग।
कोरोमंडल तट: इस क्षेत्र में वर्षा मुख्य रूप से लौटते हुए मानसून (उत्तर-पूर्वी मानसून) से होती है, जो इसे बाकी भारत से अलग बनाता है। यहां वर्षा की परिवर्तिता मध्यम से उच्च होती है।
पंजाब: यह क्षेत्र मॉनसून के अंत में वर्षा प्राप्त करता है और यहाँ भी वर्षा की परिवर्तिता अधिक होती है।
गुजरात: यहाँ वर्षा की मात्रा कम होती है और इसलिए वर्षा की परिवर्तिता बहुत अधिक होती है।
निष्कर्ष के तौर पर, दिए गए विकल्पों में से, उत्तर-पूर्वी राज्य ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ अत्यधिक वर्षा के कारण वार्षिक वर्षा की परिवर्तिता 20% से कम है।
54. उत्तरी गोलार्द्ध में धरातल पर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर पवनें किस दिशा में चलती हैं?
उत्तरी गोलार्द्ध में, धरातल पर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर चलने वाली पवनें दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व दिशा में चलती हैं।
पवन की दिशा का कारण
यह पवन प्रणाली पश्चिमी पवनें (Westerlies) कहलाती है। इन पवनों की दिशा निर्धारित करने वाले दो मुख्य कारक हैं:
दाब प्रवणता बल (Pressure Gradient Force): यह बल पवनों को हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर धकेलता है। इस मामले में, यह बल उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र (30∘ से 35∘ अक्षांश) से उपध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र (60∘ से 65∘ अक्षांश) की ओर पवनों को गति देता है।
कोरियोलिस प्रभाव (Coriolis Effect): पृथ्वी के घूर्णन के कारण, यह बल उत्तरी गोलार्द्ध में पवनों को उनकी मूल दिशा से दाईं ओर विक्षेपित करता है।
इन दोनों बलों के संयुक्त प्रभाव के कारण, पश्चिमी पवनें सीधे उत्तर की ओर चलने के बजाय दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर चलती हैं। इसी कारण इन पवनों को ‘पश्चिमी’ कहा जाता है, क्योंकि ये पश्चिम दिशा से आती हैं।
55. पंचगंगा तथा कोयना सहायक नदियाँ हैं
पंचगंगा तथा कोयना नदियाँ कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं।
पंचगंगा: यह महाराष्ट्र में बहने वाली एक नदी है, जो कोल्हापुर शहर के पास कृष्णा नदी में मिलती है।
कोयना: यह भी महाराष्ट्र में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है, जिस पर कोयना बांध बनाया गया है। यह सतारा के पास कराड़ में कृष्णा नदी से मिलती है।
56. ‘मिष्टी’ (MISHTI) पहल किस प्रकार के वनों के संरक्षण से संबंधित है?
‘मिष्टी’ (MISHTI) पहल मैंग्रोव वन के संरक्षण से संबंधित है।
मुख्य बिंदु
यह पहल भारत के समुद्र तटों और खारे पानी के किनारों पर मैंग्रोव वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी।
‘मिष्टी’ का पूरा नाम है: Mangrove Initiative for Shoreline Habitat & Tangible Incomes (तटरेखा निवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल)।
57. निम्नलिखित तेल क्षेत्रों में से कौनसा ब्रह्मपुत्र घाटी में अवस्थित नहीं है ?
ब्रह्मपुत्र घाटी में अलियाबेट तेल क्षेत्र अवस्थित नहीं है।
विवरण
अलियाबेट तेल क्षेत्र गुजरात राज्य में खंभात की खाड़ी के पास स्थित है।
दिए गए अन्य तेल क्षेत्र ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित हैं:
लखीमपुर: असम में स्थित है।
नाहरकटिया: असम में स्थित एक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है।
रुद्रसागर: असम में स्थित एक बड़ा तेल क्षेत्र है।
ये सभी क्षेत्र भारत के प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों में से हैं, लेकिन अलियाबेट ब्रह्मपुत्र घाटी के बजाय पश्चिमी भारत में स्थित है।
61. भारत के वे चार राज्य कौनसे थे जिनका वित्त वर्ष 2023 में स्थिर कीमतों पर = (2011-12 से 100) कुल औद्योगिक सकल राज्य जोड़े गये मूल्य में लगभग –
वित्त वर्ष 2023 में स्थिर कीमतों (2011-12 से 100) पर कुल औद्योगिक सकल राज्य जोड़े गए मूल्य (GVA) में सर्वाधिक योगदान देने वाले भारत के चार राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, और तमिलनाडु थे।
सही विकल्प है: (4) गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु
62. ‘संभावित सेवा उपक्षेत्रों की पहचान’ पर एक वर्किंग पेपर में नीति आयोग ने सेवाओं को उनकी कार्य प्रगति के आधार पर चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। निम्न में से सही क्षेत्रों का चयन कीजिए –
नीति आयोग द्वारा ‘संभावित सेवा उपक्षेत्रों की पहचान’ पर जारी वर्किंग पेपर में, सेवाओं को उनकी प्रगति के आधार पर चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:
बचाव के क्षेत्र (Redeem): वे क्षेत्र जो वर्तमान में कमज़ोर प्रदर्शन कर रहे हैं और जिन्हें पुनरुद्धार की आवश्यकता है।
गति बढ़ाने वाले क्षेत्र (Accelerate): वे क्षेत्र जिनमें वृद्धि की उच्च क्षमता है और जिन्हें बढ़ावा देने की ज़रूरत है।
परिवर्तन के क्षेत्र (Transform): वे क्षेत्र जिनमें महत्त्वपूर्ण नीतिगत बदलावों और नवाचारों के माध्यम से बड़ा परिवर्तन लाने की क्षमता है।
अप्रयुक्त क्षेत्र (Untapped): वे क्षेत्र जिनमें विकास की असीमित संभावनाएँ हैं लेकिन जिनका अभी तक पूरी तरह से दोहन नहीं हुआ है।
दिए गए विकल्पों में से, सही संयोजन (2) बचाव, गति बढ़ाना, परिवर्तन और अप्रयुक्त के क्षेत्र है।
63. वर्ष 2023-24 में भारत के कुल अंगूर उत्पादन में 67 प्रतिशत से अधिक का योगदान करने वाला राज्य कौनसा है?
64. आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत के कपड़ा निर्यात के संदर्भ में निम्न में से कौनसा/से कथन सही है / हैं?
- कथन I सही है: भारत वैश्विक स्तर पर कपड़ा और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है।
- कथन II गलत है: आर्थिक समीक्षा के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 में कपड़ा एवं परिधान (हस्तशिल्प सहित) का भारत के कुल निर्यात में योगदान लगभग 8.21% रहा। यह 12% नहीं है।
- कथन III सही है: वर्ष 2023 में, कपड़ा और परिधान में भारत की बाज़ार हिस्सेदारी वैश्विक स्तर पर 3.9% थी। लेकिन, वस्त्र मंत्रालय की एक अन्य प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कुछ सूत्रों ने 7% की हिस्सेदारी का उल्लेख किया है, फिर भी छठे सबसे बड़े निर्यातक होने और कुल निर्यात में योगदान के संदर्भ में, कथन I और III सबसे सटीक हैं, विशेष रूप से आर्थिक समीक्षा के संदर्भ में।
65. वर्ष 2025-26 के केन्द्रीय बजट में घोषित प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना देश के कम उत्पादकता वाले कितने जिलों में लागू की जाएगी ?
2025-26 के केंद्रीय बजट में घोषित प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना 100 जिलों में लागू की जाएगी।
यह योजना उन जिलों पर केंद्रित होगी जिनकी कृषि उत्पादकता कम है, फसल सघनता कम है और किसानों को ऋण की उपलब्धता औसत से कम है। इसका उद्देश्य इन जिलों में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में विकास को गति देना है।
66. नेहरू के नेतृत्व में आयोजित एशियाई संबंध सम्मेलन के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें
I. यह 1947 में आयोजित किया गया था।
II. यह भारत के स्वाधीनता से पहले आयोजित किया गया था।
- कथन I: यह 1947 में आयोजित किया गया था।
- यह कथन सही है। सम्मेलन 23 मार्च से 2 अप्रैल, 1947 तक नई दिल्ली में हुआ था।
- कथन II: यह भारत के स्वाधीनता से पहले आयोजित किया गया था।
- यह कथन भी सही है। भारत को 15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, जो सम्मेलन के बाद की तारीख है।
67. निम्नलिखित में से कौनसा कथन भारत सरकार अधिनियम, 1919 के बारे में सही नहीं हैं ?
- गवर्नर-जनरल की परिषद्: भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत, गवर्नर-जनरल की कार्यकारी परिषद् को वायसराय की कार्यकारी परिषद् के रूप में जाना जाता था। इसका उल्लेख वायसराय और उसकी परिषद् के रूप में किया जाता था।
- सर्वोच्च परिषद्: “गवर्नर-जनरल की सर्वोच्च परिषद्” की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी।
- अन्य कथन सही हैं:
- गवर्नर-जनरल का प्रभार: भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत, गवर्नर-जनरल विदेश और राजनीतिक विभागों का प्रभार अपने पास रखते थे।
- नियुक्ति: गवर्नर-जनरल की परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति भारत के लिए राज्य सचिव की सिफारिश पर होती थी।
- वायसराय के रूप में गवर्नर जनरल: गवर्नर-जनरल को वायसराय के रूप में ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच संपर्क का माध्यम माना जाता था।
68. राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कोष के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें –
(I) इसका प्रशासन एक कार्यकारी परिषद् द्वारा किया जाता है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है।
(II) कोष की कार्यकारी परिषद् का सचिव चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है।
(III) कोष को संघीय बजट से कोई सहयोग नहीं मिलता।
यह प्रश्न राष्ट्रीय रक्षा कोष (National Defence Fund) के बारे में है, न कि ‘राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कोष’ के। इस संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं:
कथन I: इसका प्रशासन एक कार्यकारी परिषद् द्वारा किया जाता है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है।
यह कथन सही है। राष्ट्रीय रक्षा कोष का प्रशासन एक कार्यकारी परिषद् द्वारा किया जाता है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।
कथन II: कोष की कार्यकारी परिषद् का सचिव चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है।
यह कथन गलत है। कोष की कार्यकारी परिषद् का सचिव रक्षा मंत्रालय का सचिव होता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) इसका सदस्य हो सकता है, लेकिन सचिव नहीं होता।
कथन III: कोष को संघीय बजट से कोई सहयोग नहीं मिलता।
यह कथन सही है। राष्ट्रीय रक्षा कोष स्वैच्छिक दान से प्राप्त होता है और इसे सरकारी बजट से कोई आवंटन नहीं मिलता है।
उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर, केवल I और III सही हैं।
अतः, सही विकल्प (1) केवल I और III सही है।
69. निम्नलिखित में से कौनसा अनुच्छेद/खंड / उपखंड छियासीवें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया ?
- यह संशोधन 2002 में किया गया था।
- इस खंड के तहत, माता-पिता या अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।
- इसी संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने के लिए अनुच्छेद 21ए भी जोड़ा गया था, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है।
70. निम्नांकित में से 18 वीं लोकसभा चुनाव में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल को पहचानिए –
मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल की पहचान करने के लिए, हमें 18वीं लोकसभा चुनाव के समय की स्थिति देखनी होगी। चुनाव आयोग के अनुसार, अप्रैल 2025 तक, भारत में कुछ प्रमुख राष्ट्रीय दल हैं।
दिए गए विकल्पों में से, नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP) एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल है।
नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP): इसे जून 2019 में राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला था।
अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक: यह एक राज्य स्तरीय दल है।
इंडियन नेशनल लोक दल: यह हरियाणा का एक क्षेत्रीय दल है।
अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (AITC): चुनाव आयोग द्वारा अप्रैल 2025 में इसका राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया था, क्योंकि यह लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय दल के मापदंडों को पूरा नहीं कर पाई।
इस प्रकार, 18वीं लोकसभा चुनाव के समय दिए गए विकल्पों में से केवल नेशनल पीपुल्स पार्टी ही मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल थी।
71. 2024 के आम चुनाव (लोकसभा) में भाग लेने वाले राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौनसा कथन गलत है ?
दिए गए कथनों में से कथन (3) गलत है।
कथन (3): चुनाव में 47 राज्य स्तरीय दलों ने भाग लिया। (गलत)
2024 के लोकसभा चुनाव में 55 मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों ने भाग लिया था। इसलिए, यह कथन गलत है।
अन्य कथनों का सत्यापन
कथन (1): चुनाव में 6 राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया। (सही)
2024 के आम चुनाव में चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय दल थे: भारतीय जनता पार्टी (BJP), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC), बहुजन समाज पार्टी (BSP), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (CPI-M), नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP) और आम आदमी पार्टी (AAP)।
कथन (2): चुनाव में 390 मान्यता प्राप्त (अपंजीकृत) दलों ने भाग लिया। (सही)
चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, 2024 के चुनाव में कई सौ पंजीकृत, लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त दलों ने भाग लिया। 390 का आंकड़ा इस बड़ी संख्या का एक हिस्सा हो सकता है।
कथन (4): चुनाव में भाग लेने वाली एक राष्ट्रीय पार्टी का चुनाव चिह्न ‘पुस्तक’ था। (सही)
नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP) एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसका चुनाव चिह्न ‘पुस्तक’ (Book) है।
72. निम्नांकित में से कौनसा कथन 25 नवम्बर, 1949 को संविधान सभा में दिए गए बी.आर. अम्बेडकर के अंतिम भाषण का अंश नहीं है?
डा. बी.आर. अम्बेडकर ने 25 नवंबर, 1949 को संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में कथन (4) का अंश शामिल नहीं किया था।
यह कथन “कर्तव्यों का उल्लेख” के बारे में है, जबकि उनके भाषण का मुख्य ध्यान स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के सिद्धांतों, राजनीतिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र के बीच संबंध और राजनीति में नायक-पूजा के खतरों पर था।
उनके भाषण के कुछ प्रमुख अंश इस प्रकार हैं:
“हमें हमारे राजनीतिक लोकतंत्र को अवश्यमेव सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना होगा।” (कथन 1) – उन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता को सामाजिक समानता के बिना अधूरा बताया।
“समता के बिना, स्वतंत्रता बहुतों पर कुछ की सर्वोच्चता उत्पन्न करेगी।” (कथन 2) – उन्होंने स्वतंत्रता और समानता के परस्पर संबंध पर जोर दिया।
“……राजनतिक में भक्ति या नायक-पूजा अवनति और अंततः तानाशाही का सुनिश्चित रास्ता है।” (कथन 3) – उन्होंने राजनीति में व्यक्ति-पूजा के खिलाफ चेतावनी दी।
जबकि मौलिक कर्तव्यों का विषय भारतीय संविधान के भाग IV-A में बाद में जोड़ा गया (42वें संशोधन, 1976 द्वारा), अम्बेडकर के अंतिम भाषण में इस विशिष्ट अंश का उल्लेख नहीं था।
73. कौनसा दबाव समूह ‘रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया’ नामक राजनीतिक दल में रूपांतरित हो गया ?
- ऑफ इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन (अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ): डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने 1942 में दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ने हेतु इस संगठन की स्थापना की थी।
- रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआई): बाद में, 1956 में डॉ. अंबेडकर द्वारा ही इस संगठन को एक राजनीतिक दल में बदलने की योजना बनाई गई, जिसे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। यह पार्टी मुख्य रूप से दलित अधिकारों और सामाजिक न्याय से जुड़ी है।
74. भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है ?
भारत के राष्ट्रपति के संबंध में दिए गए कथनों में से केवल कथन (2) सही है।
विवरण
कथन (1): “जब किसी राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के लिए महाभियोग चलाना हो, तब संसद का केवल निम्न सदन आरोप लगाएगा।” – यह गलत है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) द्वारा लगाया जा सकता है।
कथन (2): “व्यक्ति जो, मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के कारण रिक्त हुए राष्ट्रपति पद को भरने के लिए हुए चुनाव में विजयी हुआ है, पूरे पांच वर्ष की अवधि के लिए पद पर बने रहने का हकदार होगा।” – यह सही है। संविधान के अनुच्छेद 62(2) के अनुसार, राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए चुना गया व्यक्ति, अपने पद ग्रहण की तिथि से पूरे पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद पर बना रहता है।
कथन (3): “संसद के सभी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं।” – यह गलत है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होते।
कथन (4): “अपना पद संभालने से पूर्व, राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 59 के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण करता है।” – यह गलत है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण करता है। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद की शर्तों से संबंधित है, न कि शपथ से।
75. सिंधु जल संधि, 1960 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए –
- कथन I गलत है: सिंधु जल संधि पर 19 सितंबर, 1960 को कराची में हस्ताक्षर किए गए थे, नई दिल्ली में नहीं।
- कथन II गलत है: संधि 1 अप्रैल, 1960 को ही प्रभावी हो गई थी, न कि 12 जनवरी, 1961 को अनुमोदन पत्रों के आदान-प्रदान के बाद। हालाँकि, यह कराची में ही लागू हुई।
76. सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार से जुड़े संविधान के अनुच्छेद 29 (1) में, किसी समूह को अल्पसंख्यक निर्धारित करने का कौनसा आधार उल्लिखित नहीं है?
संविधान का अनुच्छेद 29 (1) भारत के नागरिकों के किसी भी वर्ग को, जिसकी अपनी एक विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार प्रदान करता है।
मुख्य विशेषताएँ
अधिकार का दायरा: यह अनुच्छेद भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है, न कि केवल अल्पसंख्यकों पर।
उद्देश्य: इसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षण प्रदान करना है।
संरक्षित तत्व: इसमें भाषा, लिपि और संस्कृति को विशिष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है।
निषेध: यह अनुच्छेद किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा संचालित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में केवल धर्म, जाति, भाषा या इनमें से किसी के भी आधार पर प्रवेश से इनकार नहीं करने का प्रावधान करता है।
अनुच्छेद 29 (1) और 29 (2) में अंतर: अनुच्छेद 29 (1) अल्पसंख्यक समूहों को अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखने का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 29 (2) प्रवेश में भेदभाव को रोकता है।
अनुच्छेद 30 से संबंध: अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 29 (1) केवल संस्कृति, भाषा और लिपि के संरक्षण के अधिकार को परिभाषित करता है।
77. किस वाद के फैसले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि पंथनिरपेक्षता संविधान के मूल ढाँचे का अंग हैं?
यह निर्णय एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ, 1994 वाद में दिया गया था।
इस ऐतिहासिक फैसले में, उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि पंथनिरपेक्षता संविधान की मूल संरचना का एक अभिन्न अंग है। इसका मतलब है कि संसद भी संविधान संशोधन के माध्यम से पंथनिरपेक्षता की इस मूल भावना को समाप्त नहीं कर सकती। इस मामले में, न्यायालय ने अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को रोकने के लिए दिशानिर्देश भी दिए।
78. भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में गलत कथनों के बारे में सही कूट चुनें-
दिए गए कथनों में से, कथन 3 और 4 गलत हैं।
सही विकल्प है: (3) 3 और 4 गलत है।
कथनों का विश्लेषण
कथन 1: यह कथन सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। यद्यपि अधिनियम के कुछ हिस्से तुरंत लागू हो गए, पर संघीय प्रावधानों और प्रांतीय स्वायत्तता जैसे मुख्य प्रावधान 1937 में ही लागू हुए।
कथन 2: यह कथन सही है। अधिनियम का मसौदा लॉर्ड लिनलिथगो के नेतृत्व वाली एक संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। इस समिति में ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों (हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स) के सदस्य शामिल थे।
कथन 3: यह कथन गलत है। अधिनियम को कानूनी शैली में लिखा गया था, लेकिन इसमें 14 भाग और 10 अनुसूचियाँ थीं, न कि 15 भाग और 30 अनुसूचियाँ।
कथन 4: यह कथन गलत है। ‘गुलाम संविधान’ (“Slavery Constitution”) का वाक्यांश जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम के लिए इस्तेमाल किया था। उन्होंने इस अधिनियम को “एक नई तरह की गुलामी का चार्टर” कहा था। नेशनल लिबरल फेडरेशन ने इस तरह का कोई नाम नहीं दिया था।
79. 2016 में अपनी ईरान यात्रा के दौरान, भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने त्रिपक्षीय व्यापार, परिवहन व पारगमन समझौते पर हस्ताक्षर किए । भारत तथा ईरान के अतिरिक्त उपर्युक्त समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला तीसरा देश कौनसा था?
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में ईरान का दौरा किया, तो भारत और ईरान के अलावा, त्रिपक्षीय व्यापार, परिवहन और पारगमन समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला तीसरा देश अफगानिस्तान था।
यह समझौता चाबहार बंदरगाह के विकास से संबंधित था, जिसका उद्देश्य भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच एक रणनीतिक पारगमन मार्ग स्थापित करना था, जो पाकिस्तान को बाईपास कर सके।
80. ऑपरेशन सिंदूर पर दिनांक 07.05.2025 को भारत के विदेश सचिव ने अपने वक्तव्य में किस अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के प्रेस वक्तव्य को इस कार्यवाही के संदर्भ में देखे जाने का जिक्र किया है?
- उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत की कार्रवाई को 25 अप्रैल, 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पहलगाम आतंकवादी हमले पर जारी किए गए बयान के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।
- सुरक्षा परिषद ने उस बयान में “आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने” की आवश्यकता पर बल दिया था।
- विदेश सचिव ने बताया कि भारत की जवाबी कार्रवाई इसी प्रतिबद्धता का हिस्सा थी।
81. इस दृष्टिकोण के अनुसार, अपराधी बालक वह है जो परिवार और समाज द्वारा निर्धारित आचार संहिता और मूल्यों को आन्तरीकृत करने में असफल हो जाता है और वास्तविकता एवं नैतिकता के सिद्धांतों के त्याग की कीमत पर सुख (खुशी) ढूंढता है। यह कहलाता है-
यह दृष्टिकोण मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण कहलाता है।
व्याख्या
मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार, बाल अपराध व्यक्ति की आंतरिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। यह सिद्धांत मानता है कि अपराध तब होता है जब एक बालक परिवार और समाज द्वारा निर्धारित नियमों और मूल्यों को आत्मसात करने में विफल रहता है।
यह फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से संबंधित है, जिसमें ईड (Id), अहम् (Ego) और परम-अहम् (Super-ego) की अवधारणाएँ शामिल हैं।
ईड सुख के सिद्धांत (pleasure principle) पर काम करता है, तत्काल संतुष्टि की मांग करता है।
परम-अहम् नैतिकता और सामाजिक मानदंडों का प्रतिनिधित्व करता है।
जब ईड प्रबल हो जाता है और परम-अहम् कमजोर रह जाता है, तो बच्चा सामाजिक नियमों को तोड़कर अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करता है, जिससे वह अपराधी बन जाता है।
यह दृष्टिकोण बाल अपराध को व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास और मानसिक स्वास्थ्य की समस्या के रूप में देखता है, न कि केवल सामाजिक या कानूनी समस्या के रूप में।
82. ‘शारीरिक विकास एव व्यवस्थित पैटर्न का अनुसरण करता है, जिसमें विकास शरीर के केन्द्रीय अक्ष से लेकर चरम सीमाओं तर्क बाहर की ओर फैलता है।’ किसी व्यक्ति में शारीरिक विकास के इस पैटर्न को कहा जाता है –
शारीरिक विकास के इस पैटर्न को समीपस्थ-दूरस्थ नियम (Proximodistal principle) कहा जाता है।
समीपस्थ-दूरस्थ नियम क्या है ?
यह सिद्धांत बताता है कि शारीरिक विकास शरीर के केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर, यानी रीढ़ की हड्डी से हाथों और पैरों की उंगलियों की ओर, बढ़ता है। उदाहरण के लिए, एक शिशु पहले अपनी भुजाओं और धड़ का उपयोग करना सीखता है और उसके बाद ही अपनी उंगलियों का उपयोग करके छोटी वस्तुओं को पकड़ने में सक्षम होता है।
मस्तकाधोमुखी नियम (Cephalocaudal principle) इसके विपरीत, यह बताता है कि विकास सिर से शुरू होकर पैर की ओर बढ़ता है।
83 एरिक्सन के मनो-सामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार, जब उत्तर-बाल्यावस्था का बच्चा नवीन ज्ञान अर्जितथा बौद्धिक कौशल सीखने हेतु परिश्रम करने के बावजूद बार-बार असफल होता है, तब उसमें कौनसे भाव विकसित होते हैं?
एरिक्सन के मनो-सामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार, जब उत्तर-बाल्यावस्था (लगभग 6 से 12 वर्ष) का बच्चा नवीन ज्ञान और बौद्धिक कौशल सीखने हेतु परिश्रम करने के बावजूद बार-बार असफल होता है, तब उसमें हीनता (inferiority) का भाव विकसित होता है।
इस अवस्था को ‘परिश्रम बनाम हीनता’ (Industry vs. Inferiority) कहा जाता है। इस चरण के दौरान, बच्चे अपने साथियों के साथ स्कूल और अन्य गतिविधियों में अपने कौशल और क्षमताओं की तुलना करते हैं। यदि वे महसूस करते हैं कि वे सफल हो रहे हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं, तो उनमें परिश्रम और दक्षता की भावना विकसित होती है। लेकिन, यदि वे बार-बार असफल होते हैं या महसूस करते हैं कि वे दूसरों से कम हैं, तो उनमें हीनता का भाव उत्पन्न होता है, जो भविष्य के विकास को प्रभावित कर सकता है।
84. ग्राहम वाल्स के अनुसार, संभावनाओं को तलाशना, विचार उत्पन्न करना, अस्पष्टता और लचीलेपन को आने देना, ये सृजनात्मक चिंतन प्रक्रिया के किस चरण के अंतर्गत आते हैं ?
ग्राहम वाल्स के अनुसार, संभावनाओं को तलाशना, विचार उत्पन्न करना, अस्पष्टता और लचीलेपन को आने देना, ये सभी सृजनात्मक चिंतन प्रक्रिया के उद्भवन (Incubation) चरण के अंतर्गत आते हैं।
ग्राहम वाल्स के सृजनात्मक चिंतन के चरण
ग्राहम वाल्स ने अपनी पुस्तक द आर्ट ऑफ थॉट (The Art of Thought) में सृजनात्मक चिंतन प्रक्रिया के चार मुख्य चरण बताए हैं:
तैयारी (Preparation): इस चरण में व्यक्ति समस्या को समझता है, जानकारी इकट्ठा करता है और उस पर ध्यान केंद्रित करता है।
उद्भवन (Incubation): यह वह चरण है जब व्यक्ति समस्या से सचेत रूप से दूर हो जाता है। इस दौरान, अचेतन मन में विचारों और सूचनाओं को मिलाने की प्रक्रिया चलती रहती है। यही वह समय है जब अस्पष्टता और लचीलेपन के साथ नए विचार और संभावनाएँ उत्पन्न होती हैं।
प्रदीपन (Illumination): यह वह क्षण है जब अचानक ‘आह!’ या ‘युरेका!’ का भाव आता है और समस्या का समाधान अचानक से मन में प्रकट हो जाता है।
सत्यापन (Verification): इस अंतिम चरण में, व्यक्ति समाधान की वैधता की जांच करता है और यह सुनिश्चित करता है कि वह सही और प्रभावी है।
85. शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्यापक को सम्पूर्ण सामाजिक वातावरण और अधिगम पर उसके प्रभाव की संक्रियाओं के बारे में जानने में सहायता करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का यह योगदान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है ?
शिक्षा मनोविज्ञान का यह योगदान समूह गतिशीलता की समझ से संबंधित है।
विवरण
शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो शिक्षकों को न केवल व्यक्तिगत छात्रों को समझने में मदद करता है, बल्कि कक्षा के भीतर और बाहर के सामाजिक वातावरण को भी समझने में सहायता करता है।
समूह गतिशीलता (Group Dynamics): यह कक्षा में छात्रों के बीच संबंधों, अंतःक्रियाओं और उनके व्यवहार पर समूह के प्रभाव का अध्ययन करता है। जब एक शिक्षक यह समझता है कि सामाजिक वातावरण और समूह का व्यवहार अधिगम को कैसे प्रभावित करता है, तो वह कक्षा को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकता है।
अधिगम पर प्रभाव: एक छात्र का अधिगम केवल उसकी व्यक्तिगत क्षमताओं पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उस सामाजिक माहौल पर भी निर्भर करता है जिसमें वह सीख रहा है। जैसे, सहकर्मियों के साथ सकारात्मक संबंध और एक सहयोगी कक्षा का वातावरण अधिगम को बढ़ा सकता है। इसके विपरीत, नकारात्मक समूह गतिशीलता अधिगम में बाधा डाल सकती है।
इसलिए, शिक्षा मनोविज्ञान का यह विशिष्ट योगदान, जिसमें सामाजिक वातावरण और अधिगम पर उसके प्रभाव की समझ शामिल है, सीधे तौर पर समूह गतिशीलता से जुड़ा है।
86. जब एक शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धि पर चॉकलेट देता है, तो अधिगम के क्रिया-प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार उसके द्वारा किस प्रकार का पुनर्बलन दिया गया ?
जब एक शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धि पर चॉकलेट देता है, तो अधिगम के क्रिया-प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार यह एक प्राथमिक पुनर्बलन (primary reinforcement) है।
पुनर्बलन के प्रकार
प्राथमिक पुनर्बलन (Primary Reinforcement): यह वह पुनर्बलन है जो किसी जीव की जैविक या शारीरिक आवश्यकताओं को सीधे तौर पर पूरा करता है। ये स्वाभाविक रूप से संतोषजनक होते हैं और इन्हें सीखने की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए, भोजन, पानी और आरामदायक तापमान। इस मामले में, चॉकलेट भोजन की श्रेणी में आता है, जो एक प्राथमिक पुनर्बलन है।
द्वितीयक पुनर्बलन (Secondary Reinforcement): यह वह पुनर्बलन है जो स्वाभाविक रूप से संतोषजनक नहीं होता, लेकिन किसी प्राथमिक पुनर्बलक के साथ जुड़कर प्रभावी हो जाता है। इन्हें सीखा जाता है। उदाहरण के लिए, धन, प्रशंसा, ग्रेड या टोकन।
सामाजिक पुनर्बलन (Social Reinforcement): यह द्वितीयक पुनर्बलन का एक प्रकार है जिसमें सामाजिक स्वीकृति, प्रशंसा, मुस्कान या ध्यान शामिल होता है।
क्रमिक पुनर्बलन (Continuous Reinforcement): यह पुनर्बलन की एक अनुसूची है जिसमें किसी वांछित व्यवहार के हर बार होने पर पुनर्बलन दिया जाता है।
चूंकि चॉकलेट भोजन का एक रूप है और सीधे तौर पर एक जैविक आवश्यकता को संतुष्ट करता है, इसलिए यह प्राथमिक पुनर्बलन की श्रेणी में आता है।
87. कोहलबर्ग के अनुसार, नैतिक विकास की किस अवस्था में बालक अपने मार्गदर्शन के लिए कुछ नैतिक सिद्धांत विकसित कर लेता है, जो उसके समाज के दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं और वह उन्हें सही और गलत के निर्धारण में प्रयोग करता है ?
कोहलबर्ग के अनुसार, नैतिक विकास की जिस अवस्था में बालक अपने मार्गदर्शन के लिए नैतिक सिद्धांतों को विकसित कर लेता है, जो उसके समाज के दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं और वह उन्हें सही और गलत के निर्धारण में प्रयोग करता है, वह अवस्था कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण है।
कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत
लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के छह चरणों को तीन स्तरों में विभाजित किया है:
पूर्व-परंपरागत स्तर (Pre-conventional Level):
दण्ड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण: बच्चा दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करता है।
साधन सापेक्षवादी उन्मुखीकरण: बच्चा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियमों का पालन करता है।
परंपरागत स्तर (Conventional Level):
अच्छा लड़का – अच्छी लड़की उन्मुखीकरण: बच्चा दूसरों से अनुमोदन प्राप्त करने और अच्छा दिखने के लिए नियमों का पालन करता है।
कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण (Law and Order Orientation): इस चरण में, व्यक्ति यह मानता है कि नियमों और कानूनों को बनाए रखना समाज के सुचारू संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। वह मानता है कि समाज ने जो कानून बनाए हैं, वे सही हैं और उनका पालन करना उसका कर्तव्य है। यहाँ नैतिक निर्णय समाज के दृष्टिकोण और निर्धारित नियमों पर आधारित होते हैं।
उत्तर-परंपरागत स्तर (Post-conventional Level):
सामाजिक अनुबंध उन्मुखीकरण: व्यक्ति यह समझता है कि कानून सामाजिक समझौते हैं और उनमें बदलाव किया जा सकता है।
सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखीकरण: व्यक्ति अपने स्वयं के नैतिक सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेता है, जो सार्वभौमिक मूल्यों जैसे न्याय और मानवाधिकार पर आधारित होते हैं।
88. गिलफोर्ड के बुद्धि के त्रिविमीय मॉडल की निम्नलिखित विमाओं और मानसिक प्रक्रियाओं का कौनसा युग्म सही है ?
गिलफोर्ड के बुद्धि के त्रिविमीय मॉडल की विमाओं और मानसिक प्रक्रियाओं का सही युग्म (4) अर्थगत (शाब्दिक) प्रक्रियाएँ – विषयवस्तु है।
गिलफोर्ड का बुद्धि का त्रिविमीय मॉडल
जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि को तीन स्वतंत्र आयामों में वर्गीकृत किया, जिन्हें सामूहिक रूप से संरचना मॉडल के रूप में जाना जाता है:
संक्रिया (Operations): यह वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को सोचने के तरीके को संदर्भित करती है। इसमें मूल्यांकन, अभिसारी उत्पादन, अपसारी उत्पादन, स्मृति और संज्ञान शामिल हैं।
विषयवस्तु (Contents): यह वह जानकारी है जिस पर संक्रियाएं (सोच) लागू होती हैं। इसमें अर्थगत (शाब्दिक), आकृतिक, प्रतीकात्मक, व्यवहारिक और श्रवण जैसी श्रेणियां शामिल हैं।
उत्पाद (Products): यह संक्रियाओं और विषयवस्तु के परिणामस्वरूप मिलने वाला अंतिम परिणाम है। इसमें इकाइयां, वर्ग, संबंध, प्रणाली, परिवर्तन और निहितार्थ शामिल हैं।
दिए गए विकल्पों में, ‘अर्थगत (शाब्दिक) प्रक्रियाएँ’ विषयवस्तु श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, जबकि ‘अभिसारी चिंतन प्रक्रियाएँ’ और ‘मूल्यांकन प्रक्रियाएँ’ संक्रिया श्रेणी का हिस्सा हैं। ‘सांकेतिक प्रक्रियाएँ’ भी ‘विषयवस्तु’ से संबंधित हैं, न कि ‘संक्रिया’ से।
89. पावलोव के अधिगम के शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के अनुसार, ‘जब किसी उद्दीपक के लिए अनुबंधित अनुक्रिया प्राप्त कर ली जाती है, तो अन्य समान उद्दीपक भी उसी अनुक्रिया को प्राप्त कर सकते हैं।’ यह कहलाता है-
पावलोव के अधिगम के शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के अनुसार, जब किसी उद्दीपक के लिए अनुबंधित अनुक्रिया प्राप्त कर ली जाती है, तो अन्य समान उद्दीपक भी उसी अनुक्रिया को प्राप्त कर सकते हैं। यह उद्दीपक सामान्यीकरण (Stimulus Generalization) कहलाता है।
उद्दीपक सामान्यीकरण की व्याख्या
यह घटना तब होती है जब एक जीव किसी विशिष्ट अनुबंधित उद्दीपक (जैसे एक विशिष्ट ध्वनि) के प्रति अनुक्रिया करना सीख जाता है, और फिर वह उसी तरह के अन्य उद्दीपकों (जैसे थोड़ी भिन्न ध्वनि) के प्रति भी वैसी ही अनुक्रिया करने लगता है।
उदाहरण के लिए, अगर किसी कुत्ते को घंटी की एक विशेष टोन (अनुबंधित उद्दीपक) पर लार टपकाना सिखाया जाता है, तो उद्दीपक सामान्यीकरण के कारण वह कुत्ते को घंटी की थोड़ी ऊँची या नीची टोन पर भी लार टपकाने की अनुक्रिया करेगा।
अन्य विकल्प:
उद्दीपक प्रतिस्थापन (Stimulus Substitution): यह शास्त्रीय अनुबंध का मूल सिद्धांत है, जिसमें एक तटस्थ उद्दीपक (घंटी) को एक गैर-अनुबंधित उद्दीपक (भोजन) के साथ जोड़ा जाता है ताकि वह अनुबंधित उद्दीपक बन जाए।
स्वतःस्फूर्त पुनर्लाभ (Spontaneous Recovery): यह तब होता है जब एक विलुप्त हुई अनुबंधित अनुक्रिया कुछ समय बाद बिना किसी अतिरिक्त प्रशिक्षण के अचानक फिर से प्रकट हो जाती है।
उद्दीपक विभेदीकरण (Stimulus Discrimination): यह सामान्यीकरण के विपरीत है, जहाँ जीव केवल अनुबंधित उद्दीपक के प्रति ही अनुक्रिया करता है और अन्य समान उद्दीपकों के प्रति नहीं।
90. प्रतिभाशाली बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौनसे शैक्षिक प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है ?
प्रतिभाशाली बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधानों के संबंध में, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है (4) केवल ब, स और द।
व्याख्या
(ब) ग्रेड (कक्षा) स्किपिंग अथवा कक्षांतर प्लुति: प्रतिभाशाली बच्चों को उनकी आयु के बजाय उनकी मानसिक और संज्ञानात्मक क्षमताओं के आधार पर आगे की कक्षाओं में प्रवेश देना। यह उन्हें अधिक चुनौतीपूर्ण सामग्री के साथ जुड़ने और अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर देता है। यह एक अत्यंत उपयुक्त शैक्षिक प्रावधान है।
(स) अधिक आधारभूत कोर्स को हटाना: प्रतिभाशाली छात्र अक्सर आधारभूत अवधारणाओं को जल्दी सीख लेते हैं। इसलिए, उन्हें दोहराव वाले या बुनियादी पाठ्यक्रम से छूट देना और सीधे उन्नत विषयों पर ले जाना उपयुक्त होता है।
(द) अतिरिक्त असाइन्मेंट देना: यह प्रतिभाशाली छात्रों को व्यस्त रखने और उनकी बौद्धिक जिज्ञासा को बढ़ावा देने का एक तरीका है। यह उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार अधिक गहराई से सीखने और नई चुनौतियों का सामना करने का अवसर देता है।
(अ) कालानुक्रमित आयु के आधार पर विद्यालय में प्रवेश: यह प्रावधान प्रतिभाशाली बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यह उनकी मानसिक आयु को अनदेखा करता है और उन्हें अपनी क्षमता से कम स्तर पर रहने के लिए मजबूर कर सकता है।
(य) सामग्री को जहां तक संभव हो मूर्त रूप में प्रयुक्त करना: यह प्रावधान आम तौर पर छोटे बच्चों या उन छात्रों के लिए उपयुक्त है जिन्हें अवधारणाओं को समझने में कठिनाई होती है। प्रतिभाशाली बच्चे अमूर्त अवधारणाओं को समझने में सक्षम होते हैं, इसलिए उनके लिए यह प्रावधान आवश्यक नहीं है।
91. व्यक्तित्व के निम्नलिखित उपागमों का उनसे संबंधित मनोवैज्ञानिक के साथ मिलान कीजिए –
| मनोवैज्ञानिक | व्यक्तित्व के उपागम |
| A. एरिक्सन | 1. मानवतावादी |
| B. मास्लो | 2. शरीर रचना संबंधी |
| C. कैटेल | 3. जीवनकाल |
D. शेल्डन | 4. शीलगुण |
सही मिलान है: (1) a-3, b-1, c-4, d-2
व्याख्या
ए. एरिक्सन (E. Erikson) → 3. जीवनकाल (Lifespan): एरिक्सन का सिद्धांत मनो-सामाजिक विकास पर केंद्रित है, जो पूरे जीवनकाल में आठ चरणों में व्यक्तित्व के विकास का वर्णन करता है।
बी. मास्लो (B. Maslow) → 1. मानवतावादी (Humanistic): मास्लो को मानवतावादी मनोविज्ञान के संस्थापकों में से एक माना जाता है। उनका सिद्धांत ‘आत्म-साक्षात्कार’ और मानवीय क्षमता पर जोर देता है।
सी. कैटेल (C. Cattell) → 4. शीलगुण (Trait): रेमंड कैटेल ने व्यक्तित्व के शीलगुण सिद्धांत को विकसित किया, जिसमें उन्होंने सतह शीलगुणों (Surface Traits) और स्रोत शीलगुणों (Source Traits) के आधार पर व्यक्तित्व को मापा।
डी. शेल्डन (D. Sheldon) → 2. शरीर रचना संबंधी (Constitutional): विलियम शेल्डन ने शरीर के प्रकार (सोमेटोटाइप) और व्यक्तित्व के बीच संबंध का प्रस्ताव दिया। उन्होंने एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ जैसे शरीर प्रकारों को अलग-अलग व्यक्तित्व विशेषताओं से जोड़ा।
डैनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि (Emotional Intelligence) को पाँच प्रमुख घटकों वाले एक मिश्रित निदर्श (mixed model) के रूप में प्रस्तुत किया। यह निदर्श यह बताता है कि संवेगात्मक बुद्धि केवल भावनाओं को समझने की क्षमता नहीं है, बल्कि यह एक कौशल-आधारित दृष्टिकोण है जिसे सीखा और विकसित किया जा सकता है।
पाँच प्रमुख घटक
गोलमैन के अनुसार, संवेगात्मक बुद्धि में निम्नलिखित पाँच घटक शामिल हैं:
स्व-जागरूकता (Self-Awareness): यह अपनी भावनाओं, शक्तियों, कमजोरियों, मूल्यों और लक्ष्यों को पहचानने और समझने की क्षमता है। इसमें यह भी शामिल है कि किसी की भावनाएं दूसरों को कैसे प्रभावित करती हैं।
स्वनियमन (Self-Regulation): यह अपनी भावनाओं और आवेगों को नियंत्रित करने या प्रबंधित करने की क्षमता है। यह अनुकूलनशीलता और परिवर्तन के प्रति लचीलेपन को भी दर्शाती है।
अभिप्रेरण (Motivation): यह आंतरिक प्रेरणा और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहने की क्षमता है, जिसमें आशावाद और लचीलापन शामिल है।
सहानुभूति (Empathy): यह दूसरों की भावनाओं, आवश्यकताओं और चिंताओं को समझने और उनके प्रति संवेदनशील होने की क्षमता है। यह दूसरों के परिप्रेक्ष्य से चीजों को देखने की क्षमता है।
सामाजिक कौशल (Social Skills): यह दूसरों के साथ संबंधों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की क्षमता है। इसमें संचार, संघर्ष प्रबंधन, और दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता शामिल है।
93. किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंधित धनात्मक या ऋणात्मक प्रभाव की मात्रा कहलाती है –
किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंधित धनात्मक या ऋणात्मक प्रभाव की मात्रा अभिवृत्ति (attitude) कहलाती है।
अभिवृत्ति की व्याख्या
अभिवृत्ति किसी व्यक्ति की किसी वस्तु, विचार, व्यक्ति या स्थिति के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक मूल्यांकन की प्रवृत्ति है। यह हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है और इसमें तीन मुख्य घटक होते हैं:
संज्ञानात्मक घटक: वस्तु के प्रति हमारे विचार और विश्वास।
भावनात्मक घटक: वस्तु के प्रति हमारी भावनाएँ (जैसे पसंद या नापसंद)।
व्यवहार संबंधी घटक: वस्तु के प्रति हमारा व्यवहार।
उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ भोजन के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखता है, तो इसका मतलब है कि वह स्वस्थ भोजन को पसंद करता है (धनात्मक प्रभाव) और इसे खाने की अधिक संभावना है।
अन्य विकल्पों की व्याख्या
रूचि (Interest): यह किसी वस्तु या गतिविधि में ध्यान और संलग्नता की भावना है। यह अभिवृत्ति का एक हिस्सा हो सकती है, लेकिन यह स्वयं धनात्मक या ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है।
अभिक्षमता (Aptitude): यह किसी विशिष्ट कौशल को सीखने या हासिल करने की जन्मजात क्षमता है।
आदत (Habit): यह एक सीखा हुआ, स्वचालित व्यवहार है जो बार-बार दोहराया जाता है।
94. रचनावादी अधिगम सिद्धांत के 5-ई मॉडल का निम्नलिखित में से कौनसा चरण सीखने के सबसे सक्रिय चरण का प्रतिनिधित्व करता है तथा इसमें शिक्षार्थी एक-दूसरे के साथ अपने अनुभवों को साझा करते व चर्चा करते हैं?
रचनावादी अधिगम सिद्धांत के 5-ई मॉडल का जो चरण सीखने के सबसे सक्रिय चरण का प्रतिनिधित्व करता है और जिसमें शिक्षार्थी एक-दूसरे के साथ अपने अनुभवों को साझा करते व चर्चा करते हैं, वह है विस्तार करना (Elaborate)।
5-ई मॉडल के चरण
संलग्न करना (Engage): इस चरण में, शिक्षक छात्रों को सीखने की प्रक्रिया से जोड़ने के लिए प्रश्न पूछता है या कोई गतिविधि कराता है। इसका उद्देश्य छात्रों में जिज्ञासा और रुचि जगाना है।
खोज करना (Explore): इस चरण में, छात्र स्वयं प्रयोग करते हैं, अवलोकन करते हैं और अनुभवों के माध्यम से अवधारणाओं की खोज करते हैं।
व्याख्या करना (Explain): इस चरण में, शिक्षक छात्रों की खोजों के आधार पर अवधारणाओं की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। छात्र भी अपने शब्दों में अपनी समझ व्यक्त करते हैं।
विस्तार करना (Elaborate): यह सीखने का सबसे सक्रिय चरण है। इसमें छात्र नए ज्ञान को लागू करते हैं और अपनी समझ को गहराई देते हैं। वे अपने अनुभवों को साझा करते हैं, चर्चा करते हैं, और सीखे गए ज्ञान को नई स्थितियों में उपयोग करते हैं।
मूल्यांकन करना (Evaluate): इस अंतिम चरण में, शिक्षक और छात्र दोनों ही अधिगम प्रक्रिया और समझ का मूल्यांकन करते हैं।
95. अभिप्रेरणा के विषय में निम्नलिखित में से कौनसे कथन सही हैं?
अभिप्रेरणा के विषय में, सही कथन ब, स एवं द हैं। इसलिए सही उत्तर है (3) केवल ब, स एवं द।
कथनों का विश्लेषण
अ) अभिप्रेरणा व्यवहार के कुछ ही पक्षों को प्रभावित करती है। (गलत)
अभिप्रेरणा एक व्यापक मनोवैज्ञानिक कारक है जो व्यक्ति के व्यवहार के लगभग सभी पक्षों, जैसे सीखने, सोचने, कार्य करने और यहां तक कि भावनाओं को भी प्रभावित करती है। यह केवल कुछ सीमित क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है।
ब) अभिप्रेरणा एक बच्चे से दूसरे बच्चे में भिन्न होती है। (सही)
प्रत्येक बच्चे की आंतरिक और बाहरी प्रेरणा के स्रोत अलग-अलग होते हैं। कुछ बच्चे सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं, जबकि कुछ को बाहरी पुरस्कारों या प्रशंसा की आवश्यकता होती है। यह भिन्नता उनकी रुचियों, व्यक्तित्व और अनुभवों के कारण होती है।
स) अभिप्रेरणा की स्थिति में भावनात्मक उत्तेजना पाई जाती है। (सही)
जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है, तो वह अक्सर भावनात्मक रूप से उत्साहित या उत्तेजित महसूस करता है। यह उत्तेजना उस कार्य के प्रति उसके जुनून और उत्साह को दर्शाती है।
द) अप्रेरित विद्यार्थी आसानी से पहचानने में आ जाते हैं। (सही)
अप्रेरित विद्यार्थी अक्सर सीखने की प्रक्रिया में रुचि नहीं दिखाते, वे निष्क्रिय रहते हैं, असाइनमेंट में देरी करते हैं और कक्षा में कम भागीदारी करते हैं। उनके ये व्यवहार आसानी से पहचाने जा सकते हैं।
96. रेनिंगर और हिडी द्वारा वर्णित अभिरूचि विकास प्रतिमान की चार अवस्थाएं नीचे दी गई है।
रेनिंगर और हिडी द्वारा वर्णित अभिरुचि विकास प्रतिमान की चार अवस्थाओं का सही क्रम है: स – ब – अ – द।
यह क्रम किसी व्यक्ति में रुचि के क्रमिक विकास को दर्शाता है।
स) स्थितिपरक अभिरूचि उत्प्रेरित (Triggered Situational Interest): यह पहला चरण है। रुचि किसी बाहरी घटना या उत्तेजना से अचानक उत्पन्न होती है। जैसे, किसी फिल्म या टीवी शो को देखकर किसी विशेष विषय में अचानक रुचि पैदा होना।
ब) स्थितिपरक अभिरूचि अनुरक्षित (Maintained Situational Interest): इस चरण में, व्यक्ति बाहरी समर्थन (जैसे शिक्षक या माता-पिता के प्रोत्साहन) के कारण उस रुचि को बनाए रखता है। यह अभी भी बाहरी कारकों पर निर्भर है।
अ) उभरती व्यक्तिगत अभिरूचि (Emerging Individual Interest): इस चरण में, रुचि आंतरिक हो जाती है। व्यक्ति अब बाहरी समर्थन के बिना भी उस विषय में रुचि लेने लगता है।
द) अच्छी विकसित व्यक्तिगत अभिरूचि (Well-Developed Individual Interest): यह अंतिम और सबसे परिपक्व चरण है। व्यक्ति की रुचि एक स्थायी विशेषता बन जाती है और वह उस विषय से संबंधित गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेता है और लगातार सीखता रहता है।
97. प्रिया अपनी सहपाठी के उच्चतम अंक आने पर उससे ईर्ष्या एवं घृणा करती है किन्तु प्रत्यय में वह हमेशा अपनी सहपाठी को उच्चतम अंक आने पर बधाई देती है एवं मंगलकामना व्यक्त करती है। प्रिया द्वारा समायोजन हेतु अपनाई गई रक्षात्मक युक्ति का नाम क्या है ?
प्रिया द्वारा अपनाई गई रक्षात्मक युक्ति का नाम प्रतिक्रिया निर्माण (Reaction Formation) है।
व्याख्या
प्रतिक्रिया निर्माण एक मनोवैज्ञानिक रक्षात्मक युक्ति है जिसमें व्यक्ति अपनी अचेतन इच्छाओं, भावनाओं या आवेगों के ठीक विपरीत व्यवहार करता है। इस मामले में:
अचेतन भावना: प्रिया को अपनी सहपाठी की सफलता से ईर्ष्या और घृणा है।
प्रकट व्यवहार: वह अपनी इस अचेतन भावना को छिपाने के लिए जानबूझकर उसके विपरीत व्यवहार करती है, यानी उसे बधाई देती है और मंगलकामना करती है।
यह युक्ति व्यक्ति को उन भावनाओं से निपटने में मदद करती है जिन्हें वह स्वीकार नहीं कर सकता या समाज द्वारा अस्वीकार्य मानता है।
अन्य विकल्पों का विवरण
उदात्तीकरण (Sublimation): इसमें व्यक्ति अपनी सामाजिक रूप से अमान्य इच्छाओं या आवेगों को सामाजिक रूप से स्वीकार्य और रचनात्मक गतिविधियों में बदल देता है। जैसे, एक आक्रामक व्यक्ति का बॉक्सर बन जाना।
युक्तिकरण (Rationalization): इसमें व्यक्ति अपने व्यवहार या भावनाओं के लिए तार्किक, लेकिन झूठे कारण बताता है, ताकि वह स्वयं को और दूसरों को समझा सके। जैसे, ‘लोमड़ी और अंगूर’ की कहानी।
रूपांतरण (Conversion): इसमें मानसिक संघर्ष या तनाव शारीरिक लक्षणों में बदल जाता है। जैसे, परीक्षा के तनाव के कारण अचानक हाथ-पैर में दर्द होना।
98. निम्नलिखित में से कौनसा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में सही नहीं है ?
शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में कथन (3) सही नहीं है।
व्याख्या
यह एक साध्य है, साधन नहीं। (गलत)
शिक्षा मनोविज्ञान स्वयं में कोई लक्ष्य (साध्य) नहीं है। यह एक साधन (tool) है जिसका उपयोग शिक्षकों द्वारा शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने, विद्यार्थियों को समझने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए किया जाता है। इसका अंतिम लक्ष्य (साध्य) प्रभावी शिक्षण और अधिगम है, न कि स्वयं शिक्षा मनोविज्ञान।
अन्य कथन सही हैं:
यह प्रयुक्त मनोविज्ञान की एक शाखा है। (सही) – शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में व्यावहारिक उपयोग करता है।
यह मूल्यों एवं आदर्शों की प्राप्ति में सहायता देता है। (सही) – यह छात्रों के नैतिक और सामाजिक विकास में मदद करता है, जिससे वे आदर्श नागरिक बन सकें।
यह मानवीय पक्ष को महत्वपूर्ण मानते हुए शिक्षण-अधिगम में सहायता करता है। (सही) – यह शिक्षार्थी के व्यक्तिगत, भावनात्मक और सामाजिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है, ताकि अधिगम प्रक्रिया अधिक मानवीय और प्रभावी हो सके।
99. सूची I (लक्षणों के वितरण) को सूची II (लक्षणों की श्रेणी) से मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए
| सूची I (लक्षणों के वितरण) | सूची II (लक्षणों की श्रेणी) |
| A. सामान्य जनसंख्या में व्यापक रूप से वितरित लक्षण | 1. सतही लक्षण |
| B. वे लक्षण जो अद्वितीय है एवं किसी विशिष्ट व्यक्ति में विद्यमान है। | 2. स्रोत लक्षण |
| C. बाह्य व्यवहार द्वारा आसानी से पहचाने जाने वाले लक्षण | 3. अद्वितीय लक्षण |
| D. वे लक्षण जो अंतर्निहित संचरना में हैं और व्यक्तित्व के मूल का गठन करते है। | 4. सामान्य लक्षण |
सही उत्तर (1) a-4, b-3, c-1, d-2 है।
विवरण
यह मिलान रेमंड कैटेल और गॉर्डन आलपोर्ट जैसे मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के शीलगुण सिद्धांतों (Trait Theories) पर आधारित है।
A. सामान्य जनसंख्या में व्यापक रूप से वितरित लक्षण → 4. सामान्य लक्षण (Common Traits): ये ऐसे लक्षण हैं जो एक ही संस्कृति के सभी व्यक्तियों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं, हालाँकि उनकी मात्रा में भिन्नता हो सकती है। जैसे, बुद्धिमत्ता या आक्रामकता।
B. वे लक्षण जो अद्वितीय हैं एवं किसी विशिष्ट व्यक्ति में विद्यमान हैं → 3. अद्वितीय लक्षण (Unique Traits): ये लक्षण केवल एक विशेष व्यक्ति में पाए जाते हैं और उन्हें दूसरों से अलग करते हैं। ये कैटेल के सिद्धांत में वर्णित हैं।
C. बाह्य व्यवहार द्वारा आसानी से पहचाने जाने वाले लक्षण → 1. सतही लक्षण (Surface Traits): ये वे लक्षण हैं जिन्हें बाहरी व्यवहार या अभिव्यक्तियों के माध्यम से आसानी से देखा जा सकता है, जैसे कि चिंता, दयालुता या बेचैनी। कैटेल के अनुसार, ये स्रोत लक्षणों के संयोजन से बनते हैं।
D. वे लक्षण जो अंतर्निहित संरचना में हैं और व्यक्तित्व के मूल का गठन करते हैं → 2. स्रोत लक्षण (Source Traits): ये व्यक्तित्व की मूलभूत, अंतर्निहित इकाइयाँ हैं। कैटेल ने माना कि ये अधिक स्थिर और स्थायी होते हैं और सतही लक्षणों को निर्धारित करते हैं।
100. मैक्लेलैण्ड के अनुसार, जब विद्यार्थी प्रतिस्पर्धा करना और सफलता के लिए चुनौतियाँ स्वीकार करना चाहते हैं, तो यह किस प्रकार की अभिप्रेरक आवश्यकता है?
जब विद्यार्थी प्रतिस्पर्धा करना और सफलता के लिए चुनौतियाँ स्वीकार करना चाहते हैं, तो यह उपलब्धि की आवश्यकता (Need for Achievement) है।
मैक्लेलैण्ड का अभिप्रेरणा सिद्धांत
डेविड मैक्लेलैण्ड ने तीन प्रमुख अभिप्रेरक आवश्यकताओं की पहचान की जो मानव व्यवहार को संचालित करती हैं:
उपलब्धि की आवश्यकता (Need for Achievement): यह उन लोगों में पाई जाती है जो उत्कृष्टता प्राप्त करने, चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों को पूरा करने, और व्यक्तिगत सफलता के लिए लगातार प्रयास करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी क्षमताओं को साबित करने और अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए जोखिम लेते हैं।
संबद्धता की आवश्यकता (Need for Affiliation): यह लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण और घनिष्ठ संबंध बनाए रखने की इच्छा है। ऐसे लोग सामाजिक स्वीकृति, सहयोग और समूह कार्य पसंद करते हैं।
शक्ति की आवश्यकता (Need for Power): यह दूसरों को नियंत्रित करने, प्रभावित करने या उन पर अधिकार रखने की इच्छा है। ऐसे व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करके अपनी स्थिति और प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहते हैं।
दिए गए प्रश्न में, प्रतिस्पर्धा और चुनौतियों को स्वीकार करना सीधे तौर पर उपलब्धि की आवश्यकता से संबंधित है।
Topic Wise Rajasthan Gk
Online Test Series
Only In 11/-
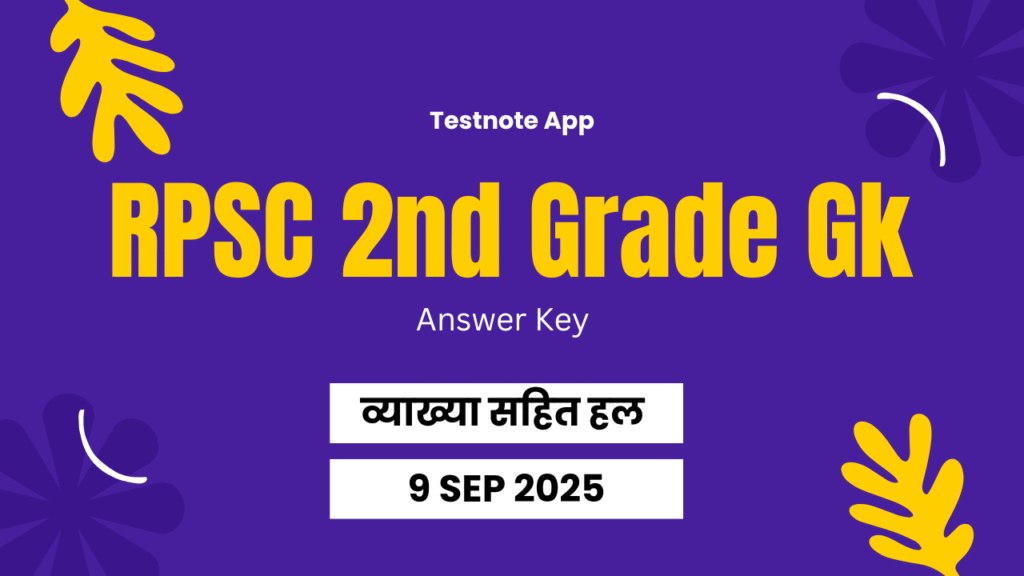
- 3rd grade 2026 sst paper answer key
- Reet Mains 2026 Math Science Paper Solution
- REET Mains L1 / L2 answer key 2026
- Rajasthan 4th Grade Paper 21 Sep 2025 2nd shift Answer Key
- Rajasthan 4th Grade Paper Answer Key 21 Sep 2025 Morning Shift
- Rajasthan 4th Grade Paper Solution 20 Sep Second Shift Answer Key
- Rajasthan 4th Grade Paper Solution 20 Sep first Shift Answer Key
- Rajasthan 4th Grade Paper Solution 19 Sep Second Shift
- Rajasthan 4th Grade Paper Solution 19 Sep First Shift
- Rajasthan police Constable Paper Solution 14 sep 2025 Evening
- Rajasthan police Constable Paper Solution 14 sep 2025 morning
- राजस्थान पुलिस टेलीकम्युनिशन पेपर 2025
- RPSC Second Grade (TGT) English 2025 Answer Key
- RPSC Second Grade 2025 Hindi Answer Key
- RPSC 2nd Grade Paper 11 Sep 2025 Answer Key Group D Gk
- RPSC 2nd Grade 2025 paper Solution 9 sep 2025 Group – C
- RPSC Second Grade Science 2025
- RPSC 2nd Grade 2025 paper Solution 8 sep 2025 Group B
- Rpsc second Grade paper Solution Group A (7 sep 2025)
